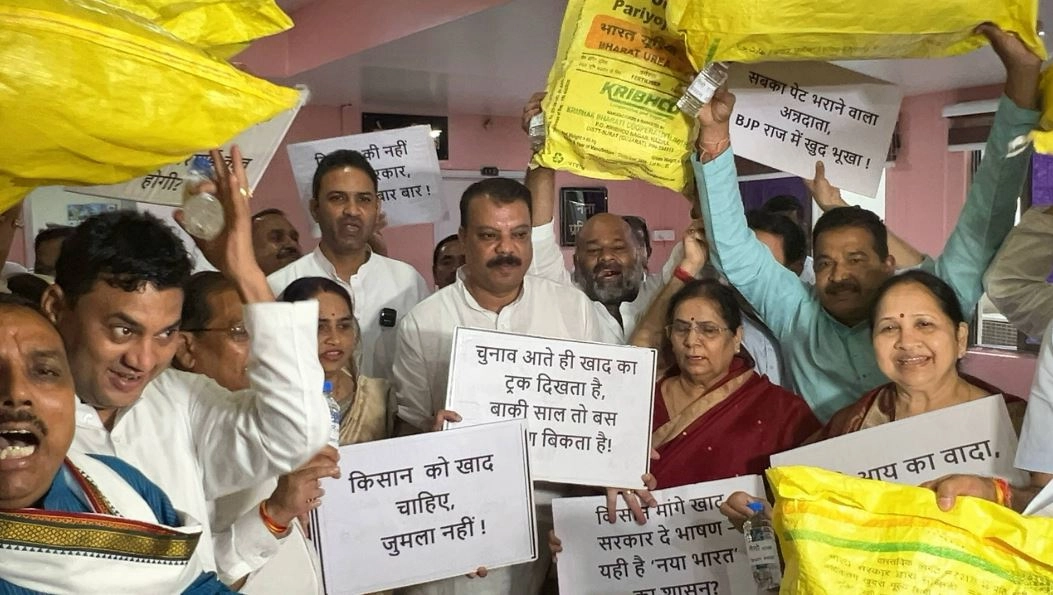महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस: जीवन परिचय

स्टोरी हाइलाइट्स
सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18फरवरी,1836 को बंगाल प्रांत स्थित ग्राम कामारपुकुर में हुआ था। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था।
महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस: जीवन परिचय
सभी धर्मों की एकता पर जोर देने वाले मानवीय मूल्यों के पोषक संत रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18फरवरी,1836 को बंगाल प्रांत स्थित ग्राम कामारपुकुर में हुआ था। महान संत एवं विचारक रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर था। गदाधर के पिता खुदीराम चट्टोपाध्याय निष्ठावान गरीब ब्राह्मण थे। गदाधर की शिक्षा तो साधारण ही हुई, किंतु पिता की सादगी और धर्मनिष्ठा का उन पर पूरा प्रभाव पड़ा। पाँच वर्ष की आयु में बालक गदाधर का विद्यारंभ संस्कार कराकर उन्हें गाँव की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा गया। पाठशाला में उनकी नित नई रचनात्मकता प्रकट होने लगी। देवी-देवताओं के चित्र बनाने और मूर्तियाँ गढ़ने में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे थे। उनकी छवि एक ऐसे होनहार बालक की बन गई, जो एक बार किसी बात को सुनने के बाद कभी भूलता नहीं हैं। इनकी बालसुलभ सरलता और मंत्रमुग्ध मुस्कान से सम्मोहित हुए बगैर कोई ना रह पाता था। जब गदाधर को ओरिएंटल सेमिनरी में भर्ती कराया गया तो किसी सहपाठी को फटा कुर्ता पहने देखकर अपना नया कुर्ता उसे दे दिया। कई बार ऐसा होने पर एक दिन माता ने गदाधर से कहा, प्रतिदिन नया कुर्ता कहां से लाऊंगी? बालक ने कहा, ठीक है, मुझे एक चादर दे दो, कुर्ते की आवश्यकता नहीं है। मित्रों की दुर्व्यवस्था देखकर संवेदनशील गदाधर के हृदय में करुणा उभर आती थी। उन्होंने पारंपरिक रूप से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की थी लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मध्यम वर्ग और बंगाली शिक्षाविदों का ध्यान अपनी ओर आकषिर्त किया।
बंगाल के एक गाँव में धार्मिकता और ईश्वर के प्रति श्रद्धा के माहौल में पालन-पोषण होने की वजह से बचपन से ही उनके मन में ईश्वर दर्शन की अभिलाषा थी। मानवता के पुजारी रामकृष्ण परमहंस को बचपन से ही विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना और भक्ति का जीवन बिताया। साधना के फलस्वरूप वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसार के सभी धर्म सच्चे हैं और उनमें कोई भिन्नता नहीं। वे ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न साधन मात्र हैं। सात वर्ष की आयु में गदाधर के भौहों के मध्य एक फोड़ा हुआ। चिकित्सक ने कहा कि बेहोश करके फोड़े को चीरना होगा। बालक ने कहा कि बेहोश करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही काटिए, मैं हिलूंगा नहीं।
सात वर्ष की अल्पायु में ही गदाधर के सर से पिता का साया उठ गया। ऐसी विपरीत परिस्थिति में पूरे परिवार का भरण-पोषण कठिन होता चला गया। आर्थिक कठिनाइयां आईं लेकिन बालक गदाधर का साहस कम नहीं हुआ। इनके बड़े भाई रामकुमार चट्टोपाध्यायकलकत्ता (कोलकाता) में एक पाठशाला के संचालक थे। वे गदाधर को अपने साथ कोलकाता ले गए। जहां पर कुछ दिनों बाद रानी रासमणि के दक्षिणेश्वर मन्दिर में पूजा के लिये नियुक्त कर दिए गए। यहीं उन्होंने माँ महाकाली के चरणों में अपने को उत्सर्ग कर दिया। वे घंटों ध्यान करते और माँ की भक्ति में ऐसे लीन रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते। वे घंटों ध्यान करते और माँ के दर्शनों के लिये तड़पते। एक दिन अर्धरात्रि को जब व्याकुलता सीमा पर पहुंची, उन जगदम्बा ने प्रत्यक्ष होकर कृतार्थ कर दिया। गदाधर अब परमहंस रामकृष्ण ठाकुर हो गये। इसी दौरान एक वृद्धा संन्यासिनी ने परमहंस जी से अनेक तान्त्रिक साधनाएँ करायीं। उनके अतिरिक्त तोतापुरी नामक एक वेदान्ती महात्मा का भी परमहंस जी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उनसे परमहंस जी ने अद्वैतज्ञान का सूत्र प्राप्त किया। उनकी महत्ता उनके त्याग, वैराग्य, पराभक्ति और उस अमृतोपदेश में है, जिससे सहस्त्रों प्राणी तार्थ हुए, जिसके प्रभाव से ब्रह्मसमाज के अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन जैसे विद्वान भी प्रभावित थे। जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक शक्ति ने नरेन्द्र जैसे नास्तिक, तर्कशील युवक को परम आस्तिक, भारत के गौरव का प्रसारक स्वामी विवेकानन्द बना दिया। उनकी उपदेश शैली सरल और भावग्राही थी। वे एक छोटे दृष्टान्त में पूरी बात कह जाते थे। स्नेह, दया और सेवा के द्वारा ही उन्होंने लोक सुधार की सदा शिक्षा दी। उन्होंने भारतीय विचार एवं संस्कृति में अपनी पूर्ण निष्ठा जताई। वे धर्मों में सत्यता के अंश को मानते थे।
रामकृष्ण जी ने मूर्तिपूजा को ईश्वर प्राप्ति का साधन अवश्य माना, किन्तु उन्होंने चिह्न एवं कर्मकाण्ड की तुलना में आत्मशुद्धि पर अधिक बल दिया। बंगाल में बाल विवाह की प्रथा है। गदाधर का भी विवाह बाल्यकाल में हो गया था। उनकी बालिका पत्नी शारदामणि जब दक्षिणेश्वर आयीं तब गदाधर वीतराग परमंहस हो चुके थे। माँ शारदामणि का कहना है- ठाकुर के दर्शन एक बार पा जाती हूँ, यही क्या मेरा कम सौभाग्य है? परमहंस जी कहा करते थे- जो माँ जगत का पालन करती हैं, जो मन्दिर में पीठ पर प्रतिष्ठित हैं, वही तो यह हैं। ये विचार उनके अपनी पत्नी माँ शारदामणि के प्रति थे। वर्ष 1859 में उनका विवाह शारदा देवी से हो गया. विवाह के समय शारदा देवी की आयु 14 वर्ष और रामकृष्ण की 23 वर्ष थी। शारदा देवी 18 वर्ष की आयु में रामकृष्ण के पास दक्षिणोर मंदिर पहुंची। शारदा देवी जब रामकृष्ण परमहंस के पास आई उस समय उन्होंने तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था। रामकृष्ण अपनी सहधर्मिणी को माँ जगदम्बा मानकर उनकी पूजा करते थे। उन दोनों का मिलन केवल आध्यात्मिक स्तर पर ही रहा। श्री रामकृष्ण ने शारदादेवी को गृहस्थी से लेकर ब्रहृमज्ञान तक सभी प्रकार से शिक्षित किया। रामकृष्ण की तरह शारदादेवी भी आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँची। शारदादेवी को आज भक्तगण माँ शारदा कहकर पुकारते हैं। रामकृष्ण की दृष्टि में पत्नी के समीप रहते हुए भी जिसके विवेक और वैराग्य अक्षुण्ण बने रहते हैं उसी को वास्तविक रूप में बह्मा में प्रतिष्ठित माना जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों को ही जो समान आत्मा के रूप में देखे और तदनुसार आचरण करे उसी को वास्तविक ब्रह्मज्ञानी माना जा सकता है।
रामकृष्ण का अन्तर्मन अत्यंत निश्छल, सहज और विनयशील था। संकीर्णताओं से वह बहुत दूर थे। अपने कार्यो में लगे रहते थे। सतत प्रयास के बावजूद रामकृष्ण का मन अध्ययन-अध्यापन में नहीं लग पाया। बीस वर्ष की अवस्था में अनवरत साधना करते-करते माता की कृपा से इन्हें परम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। काली की भक्ति में अवगाहन करके वे भक्तों को मानवता का पाठ पढाते थे। रामकृष्ण के शिष्य नाग महाशय ने गंगा तट पर जब दो लोगों को रामकृष्ण को गाली देते सुना तो क्रोधित हुए किंतु प्रभु से प्रार्थना की कि उनके मन में श्रद्धा जगाकर रामकृष्ण के भक्त बना दें। सच्ची भक्ति के कारण दोनों शाम को रामकृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। रामकृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया। एक दिन परमहंस ने आंवला मांगा। आंवले का मौसम नहीं था। नाग महाशय ढूंढते-ढूंढते जंगल में एक वृक्ष के नीचे ताजा आंवला रखा पा गये, रामकृष्ण को दिया। रामकृष्ण बोले-मुझे पता था-तू ही लेकर आएगा। तेरा विश्वास सच्चा है। रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम दिनों में समाधि की स्थिति में रहने लगे। अतरूतन से शिथिल होने लगे। शिष्यों द्वारा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की प्रार्थना पर अज्ञानता जानकर हंस देते थे। इनके शिष्य इन्हें ठाकुर नाम दिए थे। रामकृष्ण के परमप्रिय शिष्य विवेकानन्द कुछ समय हिमालय के किसी एकान्त स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आज्ञा लेने जब वे गुरु के पास गये तो रामकृष्ण ने कहा-वत्स हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूख से तडप रहे हैं। चारों ओर अज्ञान का अंधेरा छाया है। यहां लोग रोते-चिल्लाते रहें और तुम हिमालय की किसी गुफामें समाधि के आनन्द में निमग्न रहो क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकारेगी। इससे विवेकानन्द दरिद्र नारायण की सेवा में लग गये।
रामकृष्ण महान योगी, उच्चकोटि के साधक व विचारक थे। सेवा पथ को ईश्वरीय, प्रशस्त मानकर अनेकता में एकता का दर्शन करते थे। गले में सूजन को जब डाक्टरों ने कैंसर बताकर समाधि लेने और वार्तालाप से मना किया तब भी वे मुस्कराये। चिकित्सा कराने से रोकने पर भी उनके षिश्य विवेकानन्द इलाज कराते रहे। विवेकानन्द ने उनसे कहा काली मां से रोग मुक्ति के लिए आप कह दें। परमहंस ने कहा इस तन पर मां का अधिकार है, मैं क्या कहूं, जो वह करेगी मेरे लिए अच्छा ही करेगी। जीवन के अन्तिम तीस वर्षों में उन्होंने काशी, वृन्दावन, प्रयाग आदि तीर्थों की यात्रा की. उनकी उपदेश-शैली बड़ी सरल और भावग्राही थी. वे एक छोटे दृष्टान्त में पूरी बात कह जाते थे. स्नेह, दया और सेवा के द्वारा ही उन्होंने लोक सुधार की सदा शिक्षा दी। उनकी भौतिक काया 15अगस्त 1886को पंचतत्व में मिल गई। रामकृष्ण का जब उदय हुआ था, लगभग उसी समय बंगाल में ब्रह्मसमाज की स्थापना भी हुई थी। कालान्तर में रामकृष्ण द्वारा स्थापित संघ के प्रचार प्रसार से ब्रह्मसमाज के माध्यम से भारतवासियों के अर्द्ध ईसाईकरण की प्रक्रिया कम होती गई आज केवल ब्रह्मसमाज का नाम शेष है, कोई विशेष गतिविधि नहीं। इसका श्रेय रामकृष्ण परमहंस को ही देना श्रेयस्कर होगा। तदपि इसका थोड़ा श्रेय स्वामी दयानन्द को भी प्राप्त है, क्योंकि वह स्वामी दयानन्द ही थे जिन्होंने ब्रह्मसमाज के प्रवर्तन में प्रमुख बाबू केशवचन्द्र सेन को वेदों की ओर आकृष्ट किया और वास्तविक वैदिक धर्म का महत्त्व समझाया।
सपनों और हकीकत की दुनिया के बीच के संसार को सबके सामने उजागर करने के साथ सभी धर्मों को एक मान कर विश्व एकता पर बल देने का मंत्र हमारे सामने सबसे ज्यादा प्रभावी रुप से रामकृष्ण परमहंस जी ने रखा। उनका मानना था कि ‘‘मनुष्य को यदि भगवान तक पहुंचने का यत्न करना है तो उसको चाहिये कि सर्वप्रथम वह सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाये। अपने सब पूर्व संस्कारों को भुला दे। घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान ये आठों मनुष्य की आत्मा को बन्धन में रखने वाले पाश के समान हैं। भगवान तक पहुंचने के लिये इनसे मुक्त होना आवश्यक है। यज्ञोपवीत, जाति अथवा कुल का सूचक अभिमान का प्रतीक है। इसलिए यह भी पाश के समान ही है। इसी प्रकार उसको समझना चाहिए कि यह सब रुपया पैसा भी मात्र मिट्टी है, इससे अधिक कुछ भी नहीं।’’
रामकृष्ण की प्राथामिक ख्याति में यद्यपि बाबू केशवचन्द्र सेन का प्रमुख हाथ रहा था। उसका कारण कदाचित यह रहा हो कि प्रारम्भ रामकृष्ण ब्रह्मसमाज की ओर आकृष्ट होने लगे थे और केशवचन्द्र सेन को यह आभास होने लगा हो कि शीघ्र ही वे भी उनके समुदाय में सम्मिलित हो जाएंगे। किंतु ईश्वर की कृपा रही, रामकृष्ण उधर नहीं मुड़े। मानव हित के लिए रामकृष्ण ने जिन सब तत्वों की व्याख्या की है तथा कार्य रूप में उनके जीवन में जो तत्व प्रतिपादित हुए हैं, उनका प्रचार तथा मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं पारमार्थिक उन्नति के लिए जिस प्रकार सब तत्वों का प्रयोग हो सके, उन विषयों में सहायता करना, इस संघ का उद्देश्य था। इस प्रकार के संगठन द्वारा वे वेदान्त दर्शन के श्ततत्वमसिश् सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देना चाहते थे। रामकृष्ण मिशन विकासोन्मुख संस्था है और इसके सिद्धान्तों में वैज्ञानिक प्रगति तथा चिन्तन के साथ प्राचीन भारतीय अध्यात्मवाद का समन्वय इस दृष्टि से किया गया है कि यह संस्था भी पाश्चात्य देशों की भाँति जनकल्याण करने में समर्थ हो। इसके द्वारा स्कूल, कॉलेज और अस्पताल चलाये जाते हैं और कृषि, कला एवं शिल्प के प्रशिक्षण के साथ-साथ पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ भी प्रकाशित होती हैं। इसकी शाखाएँ समस्त भारत तथा विदेशों में हैं। इस संस्था ने भारत के वेदान्तशास्त्र का संदेश पाश्चात्य देशों तक प्रसारित करने के साथ ही भारतीयों की दशा सुधारने की दिशा में भी प्रशंसनीय कार्य किया है।
स्वाजी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में यह माना कि ईश्वर प्राप्ति तथा मुक्ति के अनेक रास्ते हैं और मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है, क्योंकि मानव ईश्वर का ही रूप है। स्वामी जी ने कहा कि हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं, जहाँ न वेद है, न बाइबिल है और न कुरान, लेकिन यह काम वेद, बाइबिल और कुरान के समन्वय द्वारा किया जाता है। मानवता को सीख देनी है कि सभी धर्म उस अद्वितीय धर्म की ही विभिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं, जो एकत्व है। सभी को छूट है कि उन्हें जो मार्ग अनुकूल लगे, उसको चुन लें। भारतीय धर्म के पतन के बारे में स्वामी जी ने कहा कि हमारे धर्म रसोई घर में हैं। हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में हैं।
रामकृष्ण परमहंस कहते थे- जैसे पांकाल मछली कीचड़ में ही रहती है फिर भी कीचड़ उसके शरीर से दूर रहता है वैसे ही मनुष्य को संसार में रह कर भी सांसारिक तनावों, झमेलों या वासनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। वे एक कहानी सुनाते थे। एक आदमी अपनी स्त्री को बहुत प्यार करता था। उसके बिना वह जी नहीं सकता था। एक दिन उसके गुरु ने एक दवा दी। कहा कि इसके खाते ही तुम्हारा शरीर कुछ देर के लिए मृत जैसा हो जाएगा। लेकिन तुम मरोगे नहीं। तुम्हें होश रहेगा। तुम सबकी बातें सुन सकोगे। फिर उन्होंने वैद्य को सिखाया कि तुम जाकर झूठमूठ यह कह दो कि इसे जिंदा करने के लिए किसी को अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कितना प्यार करती है। तुम तो उसके बिना जी नहीं सकते। वही हुआ। दवा खा कर वह मृत जैसा हो गया। घर में रोना- पीटना मच गया। तब वैद्य आया और बोला कि यह तो जिंदा हो जाएगा लेकिन इसके बदले किसी को जान देनी पड़ेगी। उसकी पत्नी से पूछा गया कि क्या वह अपनी जान देने को तैयार है? पत्नी ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि यह तो मर ही गए। मैं मर जाऊंगी तो इन छोटे- छोटे बच्चों को कौन देखेगा? वे कहते थे कि संसार में सब काम करो लेकिन यह जान लो कि असली घर ईश्वर के पास है। वह सब देख रहा है। मनुष्य को उसने इच्छा शक्ति दे कर छोड़ दिया है। ईश्वर देखते रहते हैं कि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करता है। रामकृष्ण परमहंस की बातें इतनी सरल होती थीं कि अनपढ़ व्यक्ति के दिल में भी वे उतर जाती थीं। वे कहते थे कि सब रुपए पैसे, परिजन और सांसारिक सुख के लिए रोते हैं। ईश्वर के लिए कौन रोता है। ईश्वर के लिए रोइए तब तो वह मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस कहते थे- मनुष्य का जन्म सिर्फ ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हुआ है। लगातार प्रार्थना करिए-- हे भगवान, हे भगवान क्या आप दर्शन नहीं देंगे? मैं आपके लिए व्याकुल हूं। लगातार प्रार्थना से उनका दिल पिघल जाता है।
परमहंस जी का जीवन द्वैतवादी पूजा के स्तर से क्रमबद्ध आध्यात्मिक अनुभवों द्वारा निरपेक्षवाद की ऊँचाई तक निर्भीक एवं सफल उत्कर्ष के रूप में पहुँचा हुआ था। उन्होंने प्रयोग करके अपने जीवन काल में ही देखा कि उस परमोच्च सत्य तक पहुँचने के लिए आध्यात्मिक विचार- द्वैतवाद, संशोधित अद्वैतवाद एवं निरपेक्ष अद्वैतवाद, ये तीनों महान श्रेणियाँ मार्ग की अवस्थाएँ थीं। ेवे एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि यदि एक को दूसरे में जोड़ दिया जाए तो वे एक दूसरे की पूरक हो जाती थीं।
किसी धनी भक्त ने एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस को एक कीमती दुशाला भेंट में दिया। स्वामी जी ऐसी वस्तुओं के शौकीन नहीं थे लेकिन भक्त के आग्रह पर उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली. उस दुशाला को वह कभी चटाई की तरह बिछाकर उसपर लेट जाते थे कभी उसे कम्बल की तरह ओढ़ लेते थे। दुशाले का ऐसा उपयोग एक सज्जन को ठीक नहीं लगा। उसने स्वामीजी से कहा दृ “यह तो बहुत मूल्यवान दुशाला है. इसका बहुत जतन से प्रयोग करना चाहिए. ऐसे तो यह बहुत जल्दी खराब हो जायेगी!” परमहंस ने सहज भाव से उत्तर दिया दृ “जब सभी प्रकार की मोह-ममता को छोड़ दिया है तो इस कपड़े से कैसा मोह करूँ? क्या अपना मन भगवान की और से हटाकर इस तुच्छ वस्तु में लगाना उचित होगा? ऐसी छोटी वस्तु की चिंता करके अपना ध्यान बड़ी बात से हटा देना कहाँ की बुद्धिमानी है?” ऐसा कहकर उन्होंने दुशाले के एक कोने को पास ही जल रहे दिए की लौ से छुआकर थोड़ा सा जला दिया और उस सज्जन से कहा दृ “लीजिये, अब न तो यह दुशाला मूल्यवान रही और न सुन्दर। अब मेरे मन में इसे सहेजने की चिंता कभी पैदा नहीं होगी और मैं अपना सारा ध्यान भगवान् की और लगा सकूँगा” वे सज्जन निरुत्तर हो गए. परमहंस ने भक्तों को समझाया कि सांसारिक वस्तुओं से मोह-ममता जितनी कम होगी, सुखी जीवन के उतना ही निकट पहुंचा जा सकेगा।
परमहंस जी का जीवन विभिन्न साधनाओं तथा सिद्धियों के चमत्कारों से पूर्ण है, किंतु चमत्कार महापुरुष की महत्ता नहीं बढ़ाते. परमहंस जी की महत्ता उनके त्याग, वैराग्य, पराभक्ति और उस अमृतोपदेश में है, जिससे सहस्त्रों प्राणी कृतार्थ हुए, जिसके प्रभाव से ब्रह्मसमाज के अध्यक्ष केशवचन्द्र सेन जैसे विद्वान भी प्रभावित थे, जिस प्रभाव एवं आध्यात्मिक शक्ति ने नरेन्द्र -जैसे नास्तिक, तर्कशील युवक को परम आस्तिक, भारत के गौरव का प्रसारक स्वामी विवेकानन्द बना दिया। तदपि न केवल पूर्वी बंगाल में अपितु देश देशान्तर में उनके असंख्य शिष्यों की ऐसी परम्परा प्रचलित है, इतने अधिक मठ और मन्दिर हैं कि कदाचित ही किसी अन्य संन्यासी के इतने शिष्य आदि हों। उनके चमत्कारों की कहानियां भी इसी संख्या में उनके शिष्यों में प्रचलित हैं।
स्वामी विवेकानन्द, जिनका पूर्व नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था, उनके ही अनन्य भक्त और शिष्य थे। उन्होंने जो कुछ भी पाया था, वह सब ठाकुर अर्थात् रामकृष्ण परमहंस की कृपा से ही प्राप्त किया था। स्वामी विवेकान्द ने विश्व भर में हिन्दुत्व का डंका बजाया था। विदेशों में वे ‘हिंदु मोंक’ के नाम से ही विख्यात रहे हैं। अपने देश में भी उनकी वैसी ही ख्याति रही है। विदेशों में हिन्दुत्व का डंका बजाने वाले कदाचित वे पहले संन्यासी थे। यद्यपि उनके बाद तो कथाकथित संन्यासियों की विदेश भ्रमण और प्रचार की गति और सीमा का कोई अन्त नहीं रहा है। कहते हैं रामकृष्ण और विवेकानंद नरेन्द्र, का मिलन नर का नारायण से, प्राचीन का नवीन से, नदी का सागर से और विश्व का भारत के साथ मिलन था।
1893 ई. में स्वामी विवेकानन्द ने शिकांगो में हुई धर्म संसद में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को भारतीय संस्कृति एवं दर्शन से अवगत कराया। धर्म संसद में स्वामी जी ने अपने भाषण में भौतिकवाद एवं आध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कही। विवेकानन्द ने पूरे संसार के लिए एक ऐसी संस्कृति की कल्पना की जो पश्चिमी देशों के भौतिकवाद एवं पूर्वी देशों के अध्यात्मवाद के मध्य संतुलन बनाने की बात कर सके तथा सम्पूर्ण विश्व को खुशियाँ प्रदान कर सके। सं.रा. अमेरिका जाने के पूर्व महाराज खेतड़ी के सुझाव पर नरेन्द्रनाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानन्द रख लिया। स्वामी जी ने ऐसे धर्म में अपनी आस्था को नकारा जो किसी विधवा के आँसू नहीं पोछ सकता व किसी अनाथ को रोटी नहीं दे सकता।
रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद ने अपने गुरु के विचारों के अनुरूप रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण कहते थे रात्रि के समय तुम आकाश में अनेक नक्षत्र देखते हो, परंतु सूर्योदय होने पर नहीं देखते। तो क्या इसी कारण तुम कह सकते हो कि दिन के समय आकश में नक्षत्र नहीं होते? हे, मानव, चूँकि तुम अपनी अज्ञान अवस्था में भगवान को देख नहीं पाते, इसी कारण यह न कहो कि भगवान नहीं हैं। अपने भौतिक शरीर को त्यागने से पूर्व उन्होंने नवयुवकों के दल का गठन किया। इन नवयुवकों में सबसे गतिशील एवं प्रखर थे- स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में इस दल ने भारत में और विदेशों में रामकृष्ण के संदेशों का प्रचार किया।
जाग्रति राजपूत



 पुराण डेस्क
पुराण डेस्क