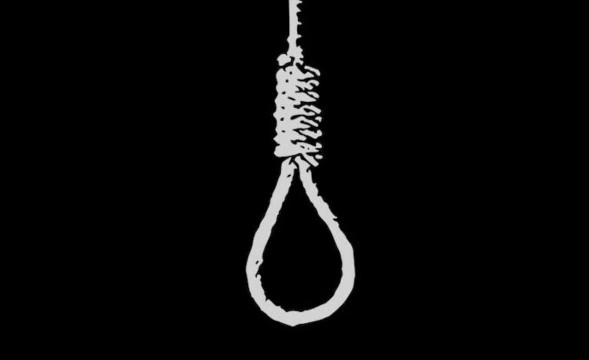मध्यप्रदेश में अतीत का रंगमंच..
आजकल मध्य प्रदेश भारत देश के जिस हिस्से में है, उसके आसपास के इलाके को प्राचीन काल में आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त के बीच में मध्यदेश था। मनुस्मृति में मनु ने मध्यदेश और आर्यावर्त को परिभाषित करते में हुए कहा है-
हिमवद्विन्ध्ययोर्मध्ये यत्प्राग्विनशनादपि ।
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तितः ।।
आ समुद्रात्तु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात् ।
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त विदुर्बुधाः ।।
जोया के बीच का हिस्सा है और वह प्रदेश जहां सरस्वती नदी का हुआ) के पूर्व में है तथा के पश्चिम में है, वह है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह जो इन दोनों पर्वतों हिमालय और विन्ध्याचल के बीच में है, उसे विद्वान लोग भयवित है।)
प्राचीन कला और नाट्य की परंपरा : पुरातात्विक साक्ष्य:
प्रागैतिहासिक शैल चित्रों से पता चलता है कि इस क्षेत्र की कला परंपरा अत्यंत प्राचीन है। भोपाल क्षेत्र के भीमबेटका, बरखेड़ा, भदभदा तथा श्यामला हिल्स; रायसेन में राम छज्जा, खरवई व पुतली करार, पन्ना, छतरपुर, खरपतिया, नौ गाँव, देवरा की गुफाएँ, सागर में आवचंद, नरयावली, हीरापुर, सिद्ध बाबा की गुफा आदि; सतना में मानिकपुर तथा चित्रकूट, ग्वालियर में कंकाली माता का टीला, शिवपुरी में कॅवला, नरसिंहगढ़ का किला, मंदसौर में मोड़ी, छिबड़ा नाला, सीताबर्डी, भानपुरा, होशंगाबाद में आदमगढ, खुदली; पचमढ़ी तथा रायगढ़ के अनेक स्थलों व दमोह, जबलपुर आदि प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख केंद्र इस प्रदेश में हैं।
पूरा मध्यप्रदेश प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का अनमोल खजाना है। रायगढ़ में बसनाझर गुफा तथा ओगना की गुफाओं में नृत्य निरत समूह तथा अनेक बायों के चित्र हैं। भरहुत की दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तथा साँची की प्रथम शताब्दी ई. की और पवाया तथा देवगढ़ आदि स्थलों में प्राप्त इसके कुछ बाद की प्रतिमाओं में नटलीला, चूड़ा महोत्सव पर नर्तन, सट्टक नामक उपरूपक के पूर्वरंग का दृश्य, सट्टक की नर्तन मंडली तथा कुतप (गायकवादक समूह) का दृश्य, बुद्ध के भौतिक अवशेषों की प्राप्ति के अवसर पर आनंद व उल्लास के क्षणों में सामूहिक नृत्य, सुधर्मा की सभा में गायन-वादन-नर्तन के दृश्य, संगीत मंडली- इन सब से ईसा के पूर्व से ईसा के पश्चात् की शताब्दियों में मध्यक्षेत्र में संपन्न सांस्कृतिक गतिविधियों विशेषतः नृत्य, नाट्य के विविध आयोजनों का परिचय मिलता है।
इनमें से भीमबेटका, पचमढ़ी और भोपाल तथा सागर (थरवई और आवचंद) के शैलाश्रय चित्रों में नर्तन (एकल और युगल) तथा समूह नृत्यों के चित्र प्राप्त होते हैं। डॉ. सुधा मलैया ने इन चित्रों में नृत्यरत स्त्रियों या पुरुषों की आकृतियों में भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में बताये गये करणों, पारियों आदि का अभिज्ञान किया है। यद्यपि भरतमुनि का नाट्यशास्त्र इन चित्रों के बहुत बाद की कृति है, पर नाट्यशास्त्र की परंपरा प्रागैतिहासिक काल में किसी न किसी रूप में भी यह इस आधार पर अवश्य माना जा सकता है।
वार में प्राप्त एक शैल चित्र में शिकार करते हुए पुरुषों का विभिन्न भाव भंगिमाओं में नर्तन जिस तरह प्रदर्शित किया गया है. यह शिकार की घटना का नाट्य रूप में अंकन ही है। सीताबेंगा की रंगशाला गुफाओं में प्राप्त शैलाधय चित्रों से जहाँ प्रागैतिहासिक काल से नृत्य और नाट्य की गतिविधियों के प्रचुर साक्ष्य तो मिलते ही हैं, पर्वतीय अंचलों व गुफाओं का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से नृत्य और नाट्य के प्रदर्शन के लिये किया जाता था इसके भी प्रमाण मध्यप्रदेश के प्राचीन पुरातात्विक सामग्री से भरपूर अनेक अंचलों में मिलते हैं।
अंबिकापुर जिले में सीताबेंगा और जोगीमारा गुफाएँ प्राचीन भारतीय शैल गुहा आश्रय मंच और गुली रंगशाला के दुर्लभ उदाहरण कहे जा सकते हैं। ये दोनों गुफाएं समुद्रतल से दो हजार फीट की ऊँचाई पर है। से दोनों के मध्य में रामगढ़ का पहाड़ है। पहाड़ के ऊपर शिव मंदिर है और उससे लगा प्राचीन दुर्ग भी है। इस दुर्ग के पास एक रघुनाथ मंदिर के भग्नावशेष हैं। सीताबेगा की गुफा का आकार 46 x 36 फीट है। इसकी दीवार पर दो शिलालेख हैं। एक शिलालेख जोगीमारा की गुफा में भी है। पहले शिलालेख में रात भर कवियों द्वारा अपनी कविता से गोष्ठी को आदीपित करने की बात कही गई है, तथा दूसरे शिलालेख में वसंत के हास और उल्लास का जिक्र है।
जोगीमारा की गुफा में प्राप्त शिलालेख में कहा गया है कि सुतनुका नाम की देवदासी यहाँ रहती थी, जिसे वाराणसी से आया हुआ रूपदक्ष देवदत्त चाहता था। ये शिलालेख दूसरी शताब्दी ई.पू. के हैं। तीनों शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं।
सीताबेंगा गुफा को जिस तरह काट कर भीतर रंगमंच और बैठने के लिये सोपानाकृति पीठ बनाये गये हैं, उनसे लगता है कि इसका इस्तेमाल चुनिंदा दर्शकों के समक्ष प्रदर्शन के लिये (इंटीमेट थियेटर के रूप में) होता था, तथा इसके बाहर के स्थल का प्रयोग खुली रंगशाला के रूप में किया जाता होगा। 1985 में संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित मेघदूत संगोष्ठी के अवसर पर डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय की नाट्य परिषद ने इसी मंच पर संस्कृत नाटक बेला, जो एक अभूतपूर्व प्रयोग रहा।
राज्यसभा की रंगशाला:-
प्राचीन काल से ही राज्यसभा में नटों, नर्तकों, नाट्य कारों को प्रश्रय दिया जाता था। मध्यप्रदेश में प्रथम शताब्दी ई.पू. में उज्जयिनी में राजा विक्रमादित्य तथा दसवीं शताब्दी में महाराज भोज कला, साहित्य और तीनों नाटक खेले गये यह इन नाटकों की प्रस्तावना से अनुमान होता है।
महाराज भोज स्वयं साहित्य, कला के मर्मज्ञ और रचनाकार थे। उन्होंने अपने समय में लुप्तप्राय हनुमन्नाटक का पुनरुद्धार कराया। उनकी राजसभा में संस्कृत के नाटककार मदन हुए, जिनकी लिखी नाटिका पारिजात मंजरी भोज ने अपने राजमहल में पत्थरों पर टँकवा कर लिखवाया था। अपनी श्रंगारमंजरी कथा नाम की किताब में भोज ने राजप्रसाद में नाट्य प्रस्तुतियाँ होने का उल्लेख भी किया है।
धार में भोज के सरस्वतीकंठाभरण नामक महल में भी रंगशाला थी। यह महल आज भोजशाला के नाम से जाना जाता है। भोज के आश्रित मदन कवि ने इस महल को शारदासम (सरस्वती का मंदिर) और भारती भवन कहा है। इसी महल में मदन कवि की नाटिका पारिजात मंजरी का भी अभिनय हुआ था। यह अभिनय धारा के राजा अर्जुन वर्मा के समय हुआ। मदन कवि की इस नाटिका को देखने के लिये धारा की जनता उमड़ पड़ी थी। सरस्वतीकण्ठाभरण नाम के महल में कविगोष्ठियाँ तथा नाटकों के प्रदर्शन होते रहते थे। इसी महल में मदन कवि की नाटिका पत्थरों पर खुदी हुई है।
भोज ने सरस्वतीकण्ठाभरण की उपाधि धारण की, इस नाम का राजमहल बनवाया तथा इस नाम से एक काव्यशास्त्र का और व्याकरण का ग्रंथ भी लिखा। सरस्वतीकण्ठाभरण के नाम से उन्होंने एक नाटक भी लिखा था। मेरुतुंगाचार्य ने अपने कथाग्रंथ प्रबन्धचिन्तामणि में बताया है कि राजा भोज अपनी राजसभा में नाटकों का अभिनय करवाते थे। ये नाटक प्रहसन कटि के विडंबनात्मक रूपक होते थे, जिन्हें 'समस्तराजविडम्बननाटक' कहा गया है।
इन में अन्य राजाओं का हास्यास्पद निरूपण रहता था। जैन ग्रंथ पुरातनप्रबन्धसंग्रह' के अनुसार भोज ने अपने समय के सिद्धों (तांत्रिकों) और योगियों पर व्यंग्य करने वाले नाटक भी करवाये थे भोज के पूर्वज सिद्धराज ने भी नाटकों के प्रयोग के लिये अलग से प्रासाद बनवाया था। मध्यकाल में त्रिपुरी (आधुनिक जबलपुर के निकट) सत्ता और संस्कृति का बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ के राजा महीपालदेव (912-44ई.) के आश्रय में संस्कृत के दो महान् नाटककार रहे राजशेखर और शेमीश्वर राजशेखर ने बालभारतम्, प्रचण्डपाण्डव, विद्धशालभज्जिका कर्पूरमञ्जरी तथा बालरामायण ये चार रूपक लिखे। इनमें से बालभारतम् का अभिनय राजा महीपाल देव की राज सभा में किया गया। क्षेमीश्वर का प्रख्यात नाटक हे चण्डकोशिक। यह राजा हरिश्चंद्र के चरित्र का निरूपण है, हिंदी के सुविदित नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सत्य हरिश्चंद्र पर इसका गहरा प्रभाव है।
दसवीं शताब्दी के आसपास ही कालंजर (वर्तमान बुंदेलखंड) और खजुराहो संस्कृति और कला साधना के केंद्र के रूप में विकसित हुए। कालंजर के राजा भीमट ने संस्कृत में पाँच नाटकों की रचना की थी। ये नाटक अब अप्राप्त हैं। कालंजर के ही दूसरे सम्राट अनंगहर्ष मायूराज हुए जिनके कवित्व की चर्चा संस्कृत के प्राचीन आचार्यों ने बार बार की है। उदात्त राघव तथा तापसी वत्सराज ये इनके रचे हुए दो नाटक हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में संस्कृत के महान नाटककार कृष्ण मिश्र हुए। इनकी अमर रचना प्रबोध चंद्रोदय नाटक के है, जिसके प्राचीन काल से ही भारत की अनेक भाषाओं में और फारसी में भी अनुवाद हुए हैं। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है। यह नाटक चंदेल राजा कीर्तिवर्मा की राजा कर्ण के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में खेला गया था।
बुंदेलखंड के प्राचीन नाटककारों में वत्सराज का नाम अविस्मरणीय है। वत्सराज कालंजर के राजा परमर्दिदेव (1163-1203 ई.), जिन्हें आल्हा काव्य में परमाल कहा गया है, के मंत्री थे। उन्होंने दुर्लभ विधाओं को ले कर संस्कृत में छह रूपक (नाटक) रचे। इनमें से किरातार्जुनीय व्यायोग का प्रदर्शन परमर्दिदेव के पुत्र त्रैलोक्य मल्ल देव के सामने हुआ। रुक्मिणीहरण ईहामृग कालंजर दुर्ग में चक्रपाणि की यात्रा के उत्सव के समय खेला गया। हास्य चूड़ामणि प्रहसन नीलकंठ की यात्रा के उत्सव के समय प्रदर्शित है। वत्सराज के रूपकों में हास्य चूड़ामणि आधुनिक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुआ है। इसके मूल संस्कृत में या हिंदी तथा अन्य भाषाओं में इसके अनुवाद को देश के सिद्धहस्त रंगकर्मियों ने मंच पर प्रस्तुत किया है।
मंदिरों का रंगमंच:-
प्राचीन काल में मंदिर या देवालय केवल देव पूजा या अनुष्ठान के ही नहीं कलात्मक तथा अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों के सक्रिय केंद्र होते थे। संगीत, नृत्य व नाट्य के प्रशिक्षण और प्रस्तुतियों की इनमें व्यवस्था रहती थी।
मध्यप्रदेश के प्राचीन मंदिरों में उज्जैन के महाकाल मंदिर में तथा ग्वालियर के निकट पद्मावती (आधुनिक पवाया) में नाट्य प्रस्तुतियाँ होने के उल्लेख प्राप्त होते हैं। मेरुतुंगाचार्य ने अपने प्रबंधचिन्तामणि में उज्जयिनी के महाकाल मंदिर के विषय में लिखा है कि राजा विक्रमादित्य इस मंदिर में नाट्यप्रयोग देखने के लिए आया करते थे। उज्जयिनी व धार के प्राचीन मंदिरों में यात्रा महोत्सवों में नाटक होते रहते थे।
मेरुतुंग ने ही राजा भोज का एक रोचक प्रसंग अपने ग्रंथ में लिखा है। धार के एक शिव मंदिर में किसी संपन्न व्यापारी ने यात्रा महोत्सव कराया। महाराज भोज को इस महोत्सव में नाटक देखने के लिये आमंत्रित किया गया। नाटक की प्रस्तावना में इस सेठ की धन सम्पदा का वर्णन सुन कर भोज चकित रह गये और उनके मन में यहाँ तक विचार आया कि क्यों न वें इस सेठ की संपदा राजसात् कर लें।
भोज ने ही अपनी श्रृंगार मंजरी कथा में मंदिरों में चलने वाली नृत्य, संगीत गायन वादन की गतिविधियों का उल्लेख किया है।
भवभूति की कर्मस्थली पद्मावती या पवाया:
इस प्रदेश के विभिन्न अंचलों में मौर्यकाल और गुप्तकाल के मन्दिरों में प्राप्त मूर्तियों से भी नृत्य व नाट्य की संपन्न गतिविधियों का संकेत मिलता है। विशेष रूप में ग्वालियर के निकट पवाया (प्राचीन पद्मपुरी) में उत्खनन से प्राप्त प्राचीन रंगमंच उल्लेखनीय है। ग्वालियर के निकट का पवाया ग्राम पुराणों में तथा शिलालेखों मं बहुचर्चित प्रसिद्ध व प्राचीन पद्मावती नगरी है।
संस्कृत के महान् नाटककार भवभूति इसी पद्मावती में रहे। कुछ विद्वानों ने तो पद्मावती या पवाया को भवभूति की जन्मस्थली भी माना है। इनके नाटक इसी पद्मावती के निकट निर्मित कालप्रियनाथ की यात्रा के महोत्सव के अवसर पर खेले गये। इनकी रचना मालतीमाधव में जिन जिन भौगौलिक स्थलों का वर्णन है, उनकी पहचान पवाया के आसपास की जा सकती है। इस नाटक के चौथे अंक में पारा और सिंधु इन दो नदियों के संगम का वर्णन है, नवम अंक में लवणा नदी वर्णित है।
मधुमती और सिन्धु नदियों के संगम का भी चित्रण भवभूति ने किया है। इस संगम पर स्वर्णबिन्दु नामक स्थान था, जिसमें भगवान् भवानीपति शंकर का मंदिर था। पवाया में प्राप्त उत्खननों से एक प्राचीन शिवलिंग मिला है। सम्भवतः भवभूति के द्वारा वर्णित स्वर्णबिन्दु स्थान यहीं रहा होगा। पारा वर्तमान पार्वती है। लवणा आज की लून नदी है। मधुमती इस समय महुवार कही जाती है।
पवाया में प्राप्त रंगमंच 108x108 हाथ के आकार का भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार ज्येष्ठ चतुरस्र मंच है। इसी पवाया में सातवीं आठवीं शताब्दी में भवभूति के नाटक खेले गये। ग्वालियर में ही बर्रइ का गोलाकार रास मंच है, जो पंद्रहवीं शताब्दी में बना। 19 वीं शताब्दी में महाराजवाड़े में नाटकघर बनाया गया, जिसका स्थापत्य रोमन शैली का है। बैजाताल में देश का पहला तैरता रंगमंच वालियर में ही है।
उपरूपकों की परंपरा तथा लोकनाट्य:
कालिदास, राजशेखर, भीमट, अनंगहर्ष, कृष्ण मिश्र, बत्तसराज जैसे महान नाटककार वर्तमान मध्यप्रदेश के प्राचीन जनपदों अवती, त्रिपुरी, कालंजर आदि में हुए इन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की परिष्कृत परंपरा को अपना कर उत्कृष्ट रूपकों (नाटक कृतियों की रचना की इन्हीं नाटककारों ने नाट्य की अन्य परंपराओं का भी उल्लेख किया है। ये परंपराएँ रूपकों के बरबस उपरूपकों की परंपराएँ हैं।
भवभूति की तीन नाटक रचनाओं पर इन लोकनाट्य परंपराओं का गहरा प्रभाव है। उन्होंने रामकथा को लेकर दो नाटक लिखे - महावीरचरितम् और उत्तररामचरितम् इन दोनों नाटकों से उस समय की रामलीला की झलक मिलती है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी एक सटक है। ऊपर हमने सट्टक के दृश्य का भरहुत में अंकन होने का उल्लेख किया है।
सट्टक उपरूपक है, जो प्राकृत या लोक भाषा में लिखा जाता है, और गीत, संगीत की प्रचुरता होती है। सटक वास्तव में प्राचीन काल का एक लोकनाट्य ही है। कर्पूर मंजरी में राजशेखर ने चर्चरी का विशद वर्णन किया है। पर्चरी भी उस काल का एक उपरूपक था। इसी तरह के अन्य उपरूपक डॉबी, भाणी या भाणिका, रासक, दण्डरासक (दांडिया रास) आदि मध्यदेश के विविध अंचलों में प्रचलित रहे हैं।
नाट्यशास्त्र की परंपरा के परवर्ती आचायों ने इनका उपरूपकों के अंतर्गत निरूपण भी किया है। ऊपर राजा भोज के द्वारा हनुमघाटक का पुनरुद्धार कराने की बात कही गई है। हनुमन्नाटक वास्तव में अत्यंत प्राचीन काल में संस्कृत में रचा गया कथागायन और लीला-शैली का नाटक है। इस नाटक में रामलीला का प्राचीन रूप मिलता है। भोज के द्वारा इस नाटक के पुनरुद्धार कराने के प्रसंग से यही आशय निकलता है कि भोज ने इस नाटक के माध्यम से रामलीला की परंपराओं को भी अपने राज्य में प्रथय दिया।
उत्तर मध्यकाल की परंपराएँ:
ग्वालियर से 12 किलोमीटर दूर बर्रई ग्राम में तोमरकालीन रंगशाला मिली है। यह सन् 1480 से 1500 ई. के बीच सक्रिय थी। इसमें नृत्य और नाटकों के प्रदर्शन होते थे। राजा मानसिंह के द्वारा बनवाई गई यह गुली रंगशाला उनके कलाप्रेम का नमूना है। यह वास्तव में गोलाकार रास मंच है, जिसे गाँव के लोग राछ कहते आये हैं। इंदौर में देवी अहत्या के शासन काल में उनकी सभा में प्रवचनकारों और कीर्तनकारों का बढ़ा सम्मान था। इसी कड़ी में यहाँ धार्मिक नाटकों की परंपरा फली फूली।
इस प्रकार मध्यप्रदेश को मध्यदेश की यह संपन्न सांस्कृतिक परंपरा विरासत में मिली है। इस के साथ ही इस प्रदेश की एक विशेषता उसकी बहुभाषीयता और बहुजातीयता भी रही है, जिसके कारण कला और साहित्य की विविध परंपराएँ यहाँ फली-फूली महाराष्ट्र समाज में मराठी नाटकों की तथा बंगाली समाज में बंगाली नाटकों की परंपरा यहाँ सक्रिय थी।
उज्जैन में महाराज विक्रमादित्य के समय से चला आ रहा संस्कृत रंगमंच के पुनराविष्कार और संस्कृत नाटकों की प्रस्तुतियों का सृजनात्मक वातावरण है। दूसरी और अभिजात और परिष्कृत रंगमंच के समानांतर उपरूपकों या लोकनाट्यों की संपन्न परंपराएँ भी इस क्षेत्र में विकसित होती रही हैं। 1956 में मध्य भारत, भोपाल, महाकौशल और विन्ध्य प्रदेश को मिला कर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया ।
इस राज्य में ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर आदि शहरों में रंगमंच और नाटक की अपनी विशिष्ट परंपराएँ उक्त पृष्ठभूमि में मौजूद थीं। (रायपुर और बिलासपुपर - ये दो जिले अब नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य में हैं)। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में लोकनाट्यों के विविध रूप भी अपनी छटा बिखेर रहे थे। इस विरासत को ले कर पचास वर्षों में कला, संस्कृति और विशेषतः रंगमंच के क्षेत्र में मध्यप्रदेश राज्य ने विशिष्ट उपलब्धियाँ हासिल की। अगले अध्यायों में हम इन पर चर्चा करेगें।
संदर्भ- (1) प्राचीन भारतीय कला में नृत्य एवं संगीत सुधा मलैया, पृ. 63,
(2) महानदी घाटी में बिखरे शैलचित्र अश्विनी केशरवानी, चौमासा, 13/ 40, पृ. 741
(3) प्राचीन भारतीय कला में नृत्य एवं संगीत- सुधा मलैया, पृ. 102-1031
(4) विवरण के लिये नाट्यम् पत्रिका का अंक 18 (भवभूति विशेषांक, फरवरी 1987) तथा महाकवि भवभूति और उनका नाट्यजगत् (सं. राधावल्लभ त्रिपाठी तथा भास्कराचार्य त्रिपाठी, 1987 द्रष्टव्य) ।
(5) उज्जयिनी का संस्कृत रंगमंच भगवतीलाल राजपुरोहित, नाट्यम्, अंक -40, पृ. 32, तथा प्रतिभा भोजराजस्य डॉ. भगवतीलाल राजपुरोहित, 1985, पृ. 151
(6) विस्तृत विवरण के लिये प्रस्तुत लेखक की नाट्यशास्त्र विश्वकोश पहला भाग तथा दूसरी परंपरा के नाटककार भवभूति ये पुस्तकें देखी जा सकती हैं।




 पुराण डेस्क
पुराण डेस्क