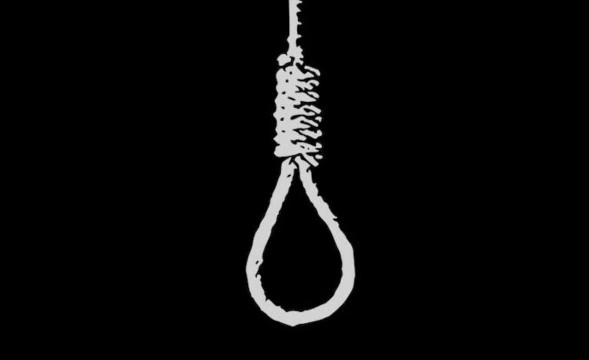भारतीय समाज :-आश्रमों का आयु अनुसार विभाजन (Division of Ashram on the basis of Age)
आज की परिस्थितियों में व्यक्ति के लिए 100 वर्ष की आयु प्राप्त करना असामान्य माना जाता है। अतीत में व्यक्तियों की औसत आयु 100 वर्ष होना तत्कालीन शुद्ध पर्यावरण व खान-पान से असंभव प्रतीत नहीं होता है। यही कारण है कि आश्रम हेतु व्यक्ति के जीवन को विविध स्तरों में विभाजित करने के लिए 100 वर्ष की मानक आयु निर्धारित की गई थी। ऋग्वेद में भी 'जीवेत शरदः शतम्' की कल्पना या भावना व्यक्त की गई है इसे दृष्टिगत रखकर ही 100 वर्ष की आयु को 25-25 वर्ष के चार कालखण्ड में विभाजित करें प्रत्येक आश्रम के लिए 25 वर्ष का काल निर्धारित किया गया यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि चारों आश्रमों का क्रम क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं अंत में संन्यास आश्रम रखा गया।
इस प्रकार प्रारंभिक 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए अनुकूल मानी गई। 25-50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम के लिए 50-75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के लिए एवं तदनन्तर मोक्ष की प्राप्ति तक संन्यास आश्रम के लिए निर्धारित की गई। इस संदर्भ में उल्लेखनीय यह है कि यह विभाजन शुद्धतः आयु से संबद्ध न होकर वस्तुतः शारीरिक व बौद्धिक क्षमताओं से संबद्ध रहा है। उदाहरणस्वरूप जन्म ग्रहण करते ही न तो बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराया जाता था और न ही ठीक 50 वर्ष पूर्ण होने पर वानप्रस्थ आश्रम में। इसी प्रकार संन्यास आश्रम में व्यक्ति 100 वर्ष पूर्ण करने तक जीवित रहेगा ही यह भी आवश्यक नहीं था। यही कारण है कि आयु के साथ-साथ शारीरिक व बौद्धिक दशाओं को भी आश्रम-व्यवस्था में प्रवेश के लिए मापदंड माना गया।
ब्रह्मचर्य आश्रम (Brahmcharya Ashram)
ब्रह्मचर्य से यहाँ तात्पर्य लैंगिक नियंत्रण नहीं है। ब्रह्म को यहाँ सांकेतिक रूप में ग्रहण किया गया है ब्रह्म का अर्थ ज्ञान, सादगी व शुद्धि से है। इस प्रकार "ब्रह्मचर्य आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति सरल, शुद्ध जीवन का निर्वाह करता है तथा ऐसे जीवन का निर्वाह करते हुए वह शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का विकास एवं ज्ञान की प्राप्ति करता है।"

ऊपर उल्लेख किया गया है कि शिशु के जन्म के साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम की सदस्यता प्राप्त नहीं हो जाती है बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था माता-पिता के संरक्षण में व्यतीत होना आवश्यक होता है यह न केवल बालक के विकास की दृष्टि से आवश्यक होता है, बल्कि इस दृष्टि से भी कि इस अवस्था में वह ज्ञान को औपचारिक रूप में अर्जित करने योग्य नहीं होता है। इस योग्य मानसिक रूप से वह विकसित हो, इसी को ध्यान में रखकर यह प्रावधान किया गया कि बालक के उपनयन संस्कार के पश्चात उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश दिया जाए। उपनयन संस्कार के लिए आयु का प्रावधान सभी वर्गों के लिए समान नहीं था। उपनयन संस्कार के पश्चात बालक पितृगृह को त्यागकर गुरु के आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम की बची हुई अवधि पूर्ण करने के लिए भेज दिया जाता था गुरु प्रायः वानप्रस्थी ऋषि हुआ करते थे। गुरु अपने आश्रम में किसी भी शिष्य के साथ
उसके वर्ण अथवा उसके पिता की सामाजिक, आर्थिक या राजनैतिक स्थिति के आधार पर भेदभाव नहीं करता था। वह आचरण, अनुशासन, दायित्व और ज्ञान प्रदान करने के लिए सबको समान दृष्टि से देखता था। ब्रह्मचर्य आश्रम कठोर नियंत्रण का आश्रम होता था इस आश्रम के माध्यम से दालकों में शारीरिक, चारित्रिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता था। इस हेतु बालक को कठिन और व्यवस्थित दिनचर्या का निर्वाह करना पड़ता था। उसे प्रातःकाल गुरु के उठने से पूर्व उठकर आश्रम की स्वच्छता, गुरु के प्रातः कालीन कार्यों के लिए समुचित व्यवस्था, आश्रम के पशुओं को चराने के लिए ले जाना और हवन के लिए जंगल से समिधा एकत्रित करके लाने का कार्य करना पड़ता था।
इसके बाद गुरु के द्वारा अध्यापन किया जाता था। मध्यान्ह में उसे निकटवर्ती ग्रहों से शिक्षा प्राप्त करने जाना पड़ता था। तदन्तर भोजन और विश्राम कर संध्या को पुनः अध्ययन, व्यायाम, यज्ञ. भोजन और गुरु की सेवा करनी पड़ती थी। इन दायित्वों का निर्वाह सब वर्णों के शिष्यों को समान रूप से करना अनिवार्य था। इस आश्रम में ब्रह्मचारी को अत्यन्त संयमित और नियमित जीवन बिताना पड़ता था। किसी भी प्रकार के सजाव, सुगंध, पुष्प, मद्यपान, मांसाहार, जूतों व छाते का उपयोग आदि ब्रह्मचारी के लिए पूरी तरह निषिद्ध था।
स्त्रियों के प्रति झुकाव भी उसके लिए वर्जित था। इस प्रकार कठोर नियंत्रण में रहने से ब्रह्मचारी में काम, क्रोध, मोह, स्वार्थ और अहं (घमंड) का विकास नहीं हो पाता था। ये दशाएँ विद्या अर्जन के अनुकूल होने के साथ-साथ व्यक्तिवादिता के स्थान पर सामाजिकता के विकास में सहयोगी रही हैं।ऋषि तथा गुरु को समाज में परम ज्ञानी माना जाता था यह वह व्यक्ति होता था जिसने स्वयं ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर अधिकतम ज्ञान अर्जित किया था और गृहस्थ आश्रम में रहकर जिसने विविध प्रकार के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किए थे। अतः ज्ञान प्रदान करने के लिए उसे सर्वथा उपयुक्त माना जाता था। यही कारण है कि वह अपने पास उपलब्ध समस्त ज्ञान सफलतापूर्वक अपने शिष्य को प्रदान करता था।
इसके साथ-साथ वह अलग-अलग वर्णों के बालकों को अपने-अपने वर्ण के कर्तव्यों का निर्वाह करने के योग्य बनाने की दृष्टि से तदनुकूल प्रशिक्षण भी देता था। जब वह यह अनुभव कर लेता था कि शिष्य ने उसके पास उपलब्ध समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है तब वह उसे ब्रह्मचर्य आश्रम त्यागने के लिए अनुकूल मान लेता था। शिक्षा पूर्ण कर लेने के प्रतीत के रूप में इस हेतु एक संस्कार -सनातन संस्कार संपादित किया जाता था। स्नातक का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान से स्नान करना होता है। इस प्रकार सांकेतिक रूप में इस संस्कार का निर्वाह कर गुरु यह घोषणा करता था कि उसके शिष्य ने उसके पास उपलब्ध ज्ञान को अर्जित कर लिया है। शिष्य भी गुरु को यथोचित गुरुदक्षिणा प्रदान कर आश्रम का त्याग करता था। आज भी स्नातक शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता है।