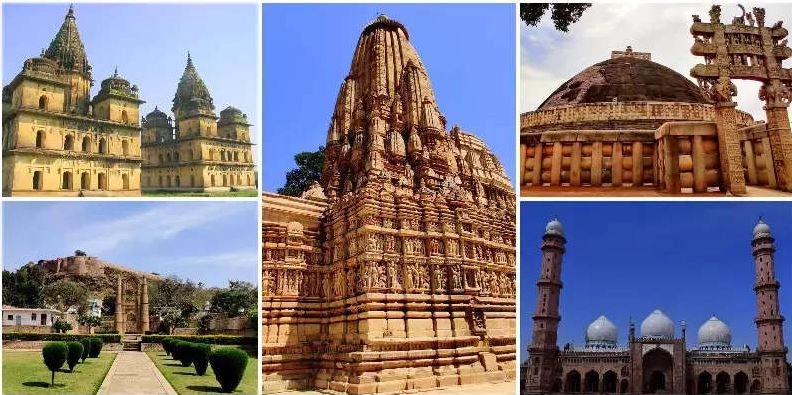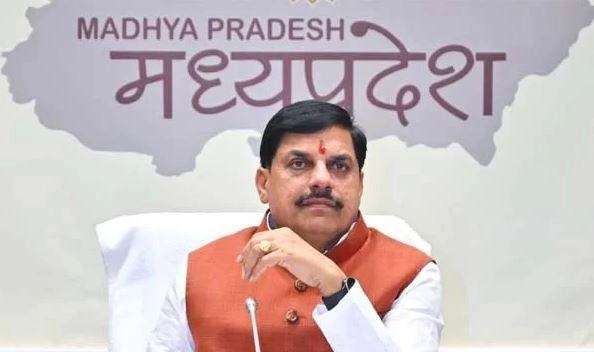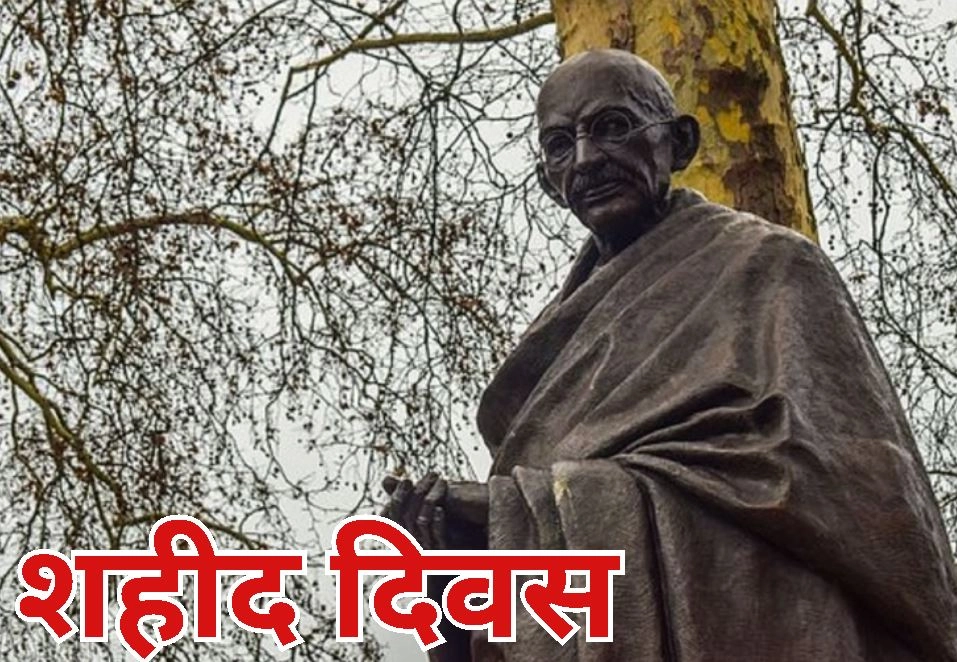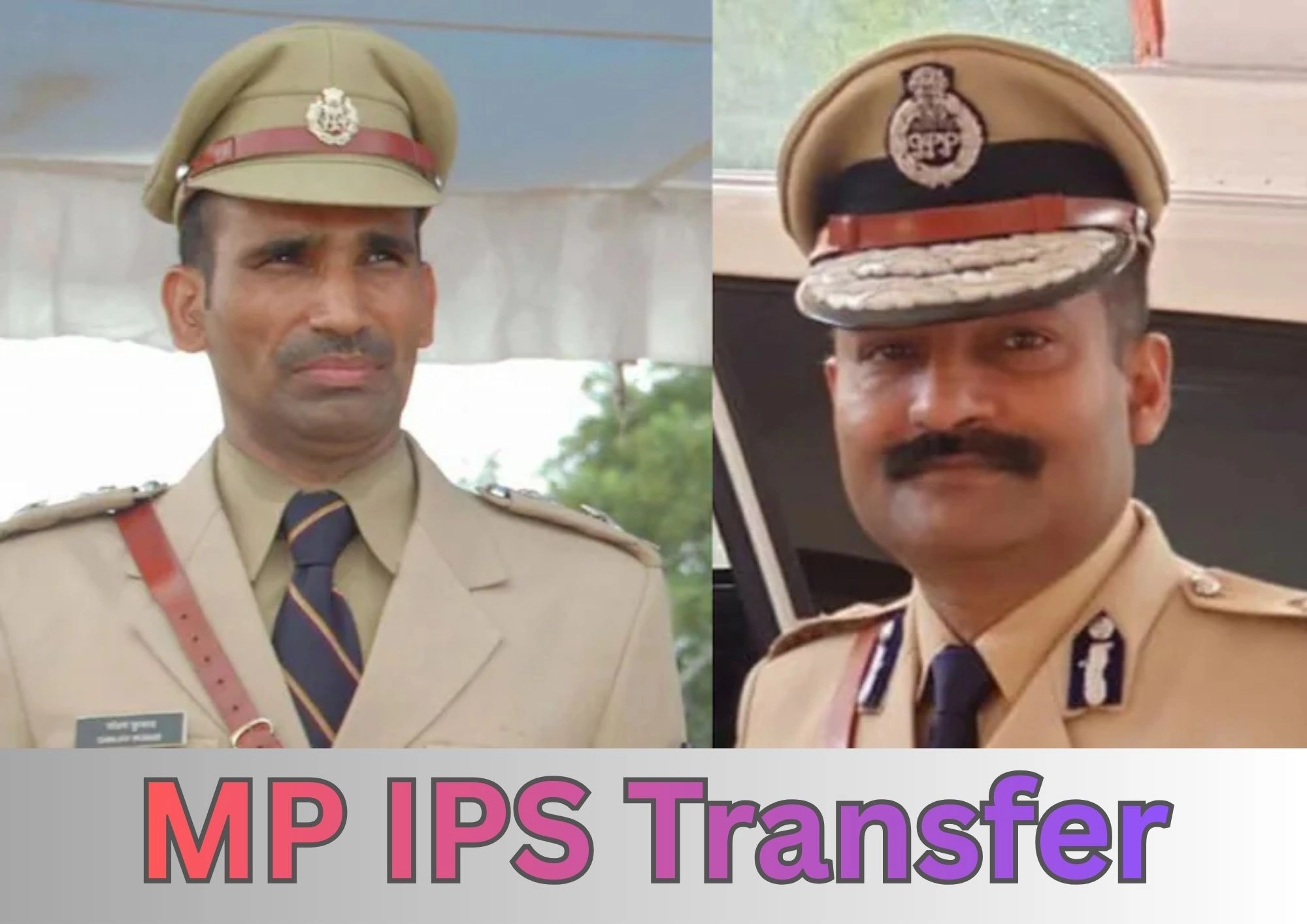भारत दाल उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश में लगभग 39.56 प्रतिशत (5.85 लाख हेक्टेयर) में मसूर(लेंटिल) की खेती की जाती है, जो क्षेत्रफल के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार क्रमशः 34.36 प्रतिशत और 12.40 प्रतिशत हैं। उत्पादन के मामले में, उत्तर प्रदेश 36.65 प्रतिशत (3.80 लाख टन) के साथ पहले और मध्य प्रदेश 28.82 के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसमें उच्चतम उत्पादकता बिहार (1124 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) और सबसे कम महाराष्ट्र (410 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) है।
यदि इसकी खेती व्यावसायिक आधार पर की जाए तो इससे काफी लाभ कमाया जा सकता है। मिश्रित फसल के रूप में इसकी खेती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। दाल के साथ सरसों, मसूर(लेंटिल) और जमसूर(लेंटिल) की सफल खेती बहुत अच्छा लाभ दे सकती है।
मसूर(लेंटिल)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
मसूर(लेंटिल) उत्पादन तकनीक |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
उन्नतशील प्रजातियाँ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
जलवायु |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
मसूर(लेंटिल) एक दीर्घ दीप्ति काली पौधा है इसकी खेती उपोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में जाड़े के मौसम में की जाती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.भूमि एवं खेत की तैयारी- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
बीज एवं बुवाई |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
बीजोपचार: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
बुआई का समय: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
पोषक तत्व प्रबंधन |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
निंदाई-गुडाई: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
पौध सुरक्षाः |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(अ) रोग : इस रोग का प्रकोप होने पर फसल की जडें गहरे भूरे रंग की हो जाती है तथा पत्तियाँ नीचे से ऊपर की ओर पीली पडने लगती है। तथा बाद में सम्पूर्ण पौधा सूख जाता है। किसी किसी पौधें की जड़े शिरा सडने से छोटी रह जाती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कालर राट या पद गलन |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
यह रोग पौधे पर प्रारंभिक अवस्था में होता है। पौधे का तना भूमि सतह के पास सड जाता है। जिससे पौधा खिचने पर बडी आसानी से निकल आता है। सड़े हुए भाग पर सफेद फफूंद उग आती है जो सरसों की राई के समान भूरे दाने वाले फफूंद के स्कलेरोषिया है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
जड़ सडन: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
यह रोग मसूर(लेंटिल) के पौधो पर देरी से प्रकट होता है, रोग ग्रसित पौधे खेत में जगह जगह टुकडों में दिखाई देते है व पत्ते पीले पड जाते है तथा पौधे सूख जाते है। जड़े काली पड़कर सड़ जाती है। तथा उखाडने पर अधिक्तर पौधे टूट जाते है व जडें भूमि में ही रह जाती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ब) रोग प्रबंधन |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
गेरुई रोग |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
इस रोग का प्रकोप जनवरी माह से प्रभावित होता है तथा संवेदनशील किस्मों में इससे अधिक क्षति होती है। इस रोग का प्रकोप होने पर सर्वप्रथम पत्तियों तथा तनों पर भूरे अथवा गुलाबी रंग के फफोले दिखाई देते है जो बाद में काले पढ जाते है रोग का भीषण प्रकोप होने पर सम्पूर्ण पौधा सूख जाता है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
रोग का प्रबंधन |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
प्रभावित फसल में 0.3% मेन्कोजेब एम-45 का 15 दिन के अंतर पर दो बार अथवा हेक्जाकोनाजोल 0.1% की दर से छिड़काव करना चाहिये। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कीट नियंत्रण |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
मसूर(लेंटिल) की फसल में मुख्य रूप से माहु तथा फली छेदक कीट का प्रकोप होता है। माहू का नियंत्रण एमिडाक्लोरपिड 150 मिलीलीटर / हेक्टेयर एवं फली छेदक हेतु इमामेक्टीन बेंजोएट 100 ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिये। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
कटाई: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
मसूर(लेंटिल) की फसल के पककर पीली पड़ने पर कटाई करनी चाहिए। पौधे के पककर सूख जाने पर दानों एवं फलियों के टूटकर झड़ने से उपज में कमी आ जाती है। फसल को अच्छी प्रकार सुखाकर बैलों के दायँ चलोर मडाई करते है तथा औसाई करके दाने को भूसे से अलग कर लेते है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
उपज: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
मसूर(लेंटिल) की फसल से 20.25 कु./ हेक्टेयर दाना एवं 30.40 कु./हेक्टेयर भूसे की उपज प्राप्त होती है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
जवलपुर कार्यशाला के दौरान निर्धारित तकनीकी बिंदु निम्नानुसार है। |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
‘‘ मसूर(लेंटिल) ‘‘ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
दाल में पाए जाने वाले पोषक तत्व और उपयोग
औसतन 100 ग्राम दाल में 25 ग्राम प्रोटीन, 1.3 ग्राम वसा होता है। इसमें 60.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3.2 ग्राम फाइबर, 68 मिलीग्राम कैल्शियम, 7 मिलीग्राम आयरन, 0.21 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन, 0.51 मिलीग्राम थाइमिन और 4.8 मिलीग्राम नियासिन होता है जो शरीर के लिए आवश्यक है। रोगों में इसके प्रयोग की बात करें तो इसका सेवन अन्य फलियों की अपेक्षा अधिक पौष्टिक पाया जाता है।
इन बीन्स को खाने से पेट के विकार दूर होते हैं। मरीजों के लिए ये दाल बेहद फायदेमंद मानी जाती है। यह एक मूत्रवर्धक है और रक्त को गाढ़ा करता है।
यह अतिसार, बहुमूत्रता, प्रदर, कब्ज और अनियमित पाचन में भी लाभकारी है। दाल के अलावा कई तरह के स्नैक्स और मिठाइयां बनाने में भी इस दाल का इस्तेमाल किया जाता है. इसका हरा और सूखा चारा मवेशियों के लिए स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है।
खेती से पहले जानने योग्य महत्वपूर्ण बातें:
- मसूर(लेंटिल) की बुवाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है, लेकिन अधिक पैदावार के लिए मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक की अवधि बुवाई के लिए आदर्श होती है।
- मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए हल्की मिट्टी की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। इसकी खेती लाल लैटेराइट मिट्टी में भी अच्छी तरह से की जा रही है।
- मटर की अच्छी फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.8-7.5 के बीच होना चाहिए।
- पौधों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है लेकिन फसल पकने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है।
- मसूर(लेंटिल) की फसल को वृद्धि के लिए 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है।
- वे क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए अच्छे होते हैं, जहाँ प्रतिवर्ष 80-100 सेमी वर्षा होती है। दूसरी ओर, बिना सिंचाई वाले वर्षा-नमी से सुरक्षित क्षेत्र में भी मसूर(लेंटिल) की खेती वर्षा आधारित परिस्थितियों में की जा सकती है।
- मसूर(लेंटिल) की फसल के साथ-साथ सरसों, मसूर(लेंटिल), जमसूर(लेंटिल) की सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। इसलिए इसकी मिश्रित तरीके से खेती की जाए तो यह अधिक लाभदायक होता है।
उन्नत किस्मों
दाल निम्नलिखित भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दाल की उन्नत किस्में हैं। उत्तर पश्चिम के मैदानों के लिए- LL-147, पंत L-406, पंत L-639, सामना, LH 84-8, L-4076, शिवालिक, पंत L-4, प्रिया, DPL-15, पंत मसूर(लेंटिल)-5, पूसा वैभव और DPL-62 मुख्य रूप से उपयोगी है। इसी तरह, AWBL-58, पंत L-406, DPL-63, Pant L-639, मलिका K-75, KLS-218 और HUL-671 किस्में उत्तरपूर्वी मैदानी इलाकों के लिए अच्छी मानी जाती हैं। इसके अलावा जेएलएस-1, सीहोर 74-3, मलिका के75, एल4076, जवाहर दाल-3, नूरीपंत एल 639 और आईपीएल-81 किस्में सेंट्रल जोन के लिए काफी उपयोगी साबित हुई हैं।
खेती कैसे करें- (खेत की तैयारी, बीज उपचार, बुवाई की विधि)
मसूर(लेंटिल) की खेती से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। इसके लिए खरीफ की फसल की कटाई के बाद 2 से 3 खड़ी जुताई करनी चाहिए, जिससे मिट्टी नाजुक और मुलायम हो जाती है। प्रत्येक जुताई के बाद, गद्दी को रोल करके मिट्टी को पीसकर समतल कर लें। यदि खेत की भूमि भारी मिट्टी वाली है, तो एक या दो और जुताई की आवश्यकता होगी। इसे अच्छी तरह से तैयार खेत में लगाएं।
मसूर(लेंटिल) की समय पर बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 30 से 35 किलोग्राम उन्नत किस्मों के बीजों की आवश्यकता होती है। देर से बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 50-60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। देर से बुवाई करने पर 40 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बोना चाहिए। मिश्रित फसलों में आमतौर पर बीज दर आधी रखी जाती है। बिजाई से पहले बीजों को थीरम या बाविस्टिन @ 3 ग्राम/किलोग्राम से उपचारित करें। इसके बाद बीजों को राइजोबियम कल्चर और दाल के फास्फोरस बैक्टीरिया पीएसबी कल्चर 5 ग्राम प्रति 10 ग्राम बीज की दर से उपचारित करें और छायादार स्थान पर सुखाकर बुवाई करें। ध्यान रहे इसे सुबह या शाम के समय लगाना चाहिए।
अच्छी उपज के लिए केले या पोरा विधि से कतारों में बुवाई करें। इस क्रिया से खेत को समतल करने के साथ ही बीजों को भी ढक दिया जाता है। पोरा विधि में देसी हल के पीछे पोरा चोंगा रखकर एक पंक्ति में बुवाई की जाती है। इसके लिए सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजों को पोरा या सीड ड्रिल द्वारा सही गहराई पर और समान दूरी पर बोया जाता है। अगेती फसल को कतारों में 30 सें.मी. की दूरी पर बोना चाहिए। देर से बुवाई करने वाली फसल के लिए पंक्तियों की दूरी 20 से 25 सेमी रखी जाती है, दाल के अपेक्षाकृत छोटे बीज के कारण यह 3-4 सेमी की उथली बुवाई के लिए उपयुक्त होती है। आजकल जीरो जुताई तकनीक से जीरो टू सीड ड्रिल से भी मसूर(लेंटिल) की बुवाई की जाती है।
उर्वरक
सिंचित स्थिति में बुवाई के समय 20 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो सल्फर, 20 किलो पोटाश और 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से।
असिंचित स्थिति में 15: 30: 10: 10 किग्रा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर को बुवाई के समय टैंक में डालने की सलाह दी जाती है। फास्फोरस को सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में देने से भी आवश्यक सल्फर तत्व की पूर्ति हो जाती है। जिंक की कमी वाली मिट्टी में जिंक सल्फेट को अन्य उर्वरकों के साथ 25 किग्रा / हेक्टेयर की दर से लगाया जा सकता है।
पहली सिंचाई टहनियों के उभरने के समय यानि बुवाई के 40 से 45 दिन बाद और दूसरी सिंचाई बीज बोने के 70 से 75 दिन बाद फली में बीज भरते समय करनी चाहिए। सावधान रहें कि पानी अधिक न हो। इसके लिए सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का प्रयोग किया जा सकता है। खेत में पट्टी बनाकर हल्की सिंचाई करने से लाभ होता है। मसूर(लेंटिल) की फसल के लिए अत्यधिक सिंचाई लाभकारी नहीं होती है। इसलिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
खरपतवार नियंत्रण
खरपतवार मसूर(लेंटिल) की फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यदि समय रहते खरपतवार नियंत्रण का ध्यान नहीं रखा गया तो उपज 30 से 35 प्रतिशत तक कम हो सकती है। इसलिए 45 से 60 दिनों के अंतराल पर खरपतवार निकालना चाहिए।
बुवाई के समय के अनुसार फरवरी और मार्च में मसूर(लेंटिल) की कटाई की जाती है। जब 70 से 80 प्रतिशत फलियाँ भूरी हो जाएँ और पौधे पीले या पक जाएँ तो फसल की कटाई करनी चाहिए।
अगर मौसम अनुकूल है और यह एक आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, यह अच्छी उपज देती है। मसूर(लेंटिल) की उपज 20 से 25 क्विंटल है।
मसूर(लेंटिल) दाल को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लवणीय, क्षारीय और जल भराव वाली मिट्टी में खेती न करें। मिट्टी दोमट और खरपतवार मुक्त होनी चाहिए ताकि बीज को सहीगहराई पर बोया जा सके।
LL 699: यह गहरे हरे पत्तों वाली जल्दी पकने वाली छोटी किस्म है। यह किस्म 145 दिनों में पक जाती है। यह किस्म फली छेदक कैटरपिलर के लिए प्रतिरोधी है। यह किस्म रतुआ और तुषार रोग के प्रति सहनशील है। इसकी औसत उपज 5 क्विंटल प्रति एकड़ है।
LL 931: फूलों और गुलाबी रंग के गहरे हरे पत्तों की किस्म। यह 146 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। यह किस्म फली छेदक कैटरपिलर के लिए प्रतिरोधी है। इसकी औसत उपज 4.8 क्विंटल प्रति एकड़ है।
अन्य राज्यों की किस्में
बॉम्बे 18: यह किस्म 130-140 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 4-4.8 क्विंटल प्रति एकड़ है।
डीपीएल 15: यह किस्म 130-140 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 5.6-6.4 क्विंटल प्रति एकड़ है।
डीपीएल 62: यह किस्म 130-140 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 6.8 क्विंटल प्रति एकड़ है।
K 75: यह किस्म 120-125 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 5.5-6.4 क्विंटल प्रति एकड़ है।
पूसा 4076: यह किस्म 130-135 दिनों में पक जाती है और कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी औसत उपज 10-11 क्विंटल प्रति एकड़ है।
बीज की गहराई
बीज की गहराई 3-4 सेमी . होनी चाहिए
बुवाई की विधि बुवाई के लिए
पोरा विधि या उर्वरक और बीज मशीन का प्रयोग करें। इसके अलावा इसे हाथ से छिड़काव करके भी बोया जा सकता है।
उर्वरक
(किलोग्राम प्रति एकड़)
|
यूरिया |
एसएसपी |
म्यूरेट ऑफ पोटाश |
|
12 |
50 |
- |
तत्व (किलोग्राम प्रति एकड़)
|
नाइट्रोजन |
फास्फोरस |
पोटाश |
|
5 |
8 |
- |
5 किलो नाइट्रोजन (12 किलो यूरिया), 8 किलो फास्फोरस (50 किलो सिंगल सुपर फास्फेट) प्रति एकड़ बुवाई के समय डालें। बिजाई से पहले बीज को राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए। यदि बुवाई से पहले बीजों को राइजोबियम से उपचारित न किया जाए तो फास्फोरस की मात्रा दोगुनी कर देनी चाहिए।
45-60 दिनों के लिए खेत को खरपतवार मुक्त रखें ताकि फसल अच्छी तरह से बढ़े और अच्छी पैदावार हो।
जलवायु परिस्थितियों के आधार पर सिंचित क्षेत्रों में इसे 2-3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक बुवाई के 4 सप्ताह बाद और दूसरा फूल आने के समय करना चाहिए। फली भरने और फूल आने की अवस्था सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण चरण है।
- हानिकारक कीट और रोकथाम
फली छेदक: यह भृंग पत्तियों, तनों और फूलों को खाता है। यह मसूर(लेंटिल) की एक खतरनाक कीट है और उपज को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसके नियंत्रण के लिए हेक्साविन @ 900 ग्राम @ 50WP @ 90Ltr पानी प्रति एकड़ फूल आने के समय छिड़काव करें। यदि आवश्यक हो, तो 3 सप्ताह के बाद तीसरा स्प्रे किया जा सकता है।
कुंगी: टहनियों, पत्तियों और फलियों पर हल्के पीले रंग के उभरे हुए धब्बे होते हैं। ये धब्बे एक समूह के रूप में दिखाई देते हैं। छोटे धब्बे धीरे-धीरे बड़े धब्बों में बदल जाते हैं। कभी-कभी प्रभावित पौधे पूरी तरह से सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करें और रोकथाम के लिए 400 ग्राम एम-45 को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें।
झुलसा रोग: यह टहनियों और फलियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे का कारण बनता है। ये धब्बे धीरे-धीरे लम्बे हो जाते हैं। कई बार बाद में ये धब्बे गोलाकार रूप ले लेते हैं। बचाव के लिए रोगमुक्त बीजों का प्रयोग करें और पौधों को नष्ट कर दें। इसके नियंत्रण के लिए 400 ग्राम बाविस्टिन को 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ मिलाकर छिड़काव करें।
सही समय पर करनी चाहिए। जब पत्तियां सूख जाती हैं और फलियां पक जाती हैं, तो फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है। देरी के कारण कैप्सूल गिर जाते हैं। इसे रेजर से काटें। अनाज को साफ करके धूप में सुखाकर 12 प्रतिशत आर्द्रता पर भंडारित करें।
देश के कुछ राज्यों में मसूर(लेंटिल) की पैराक्रॉपिंग भी की जाती है। उदाहरण के लिए झारखंड में खड़ी धान की फसल में मसूर(लेंटिल) की बुवाई की जाती है। जब धान की फसल कट जाती है, तो मसूर(लेंटिल) की फसल जोरों पर होती है। तो आइए जानते हैं कि मसूर(लेंटिल) की खेती के दौरान सिंचाई का प्रबंधन कैसे करें।
अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 55 किग्रा यूरिया, 44 किग्रा डीएपी, 85 किग्रा पोटाश एवं 25 किग्रा जिंक सल्फेट देना चाहिए।
मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन
मसूर(लेंटिल) की खेती सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रों में की जाती है। खेत की तैयारी के बाद, पलेवा द्वारा मसूर(लेंटिल) की बुवाई की जाती है। इसके बाद इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके पास पानी के पर्याप्त साधन हों तो भी फूल आने या रोपण के 40 से 45 दिन बाद सिंचाई की जा सकती है। ज्यादा पानी मसूर(लेंटिल) की फसल को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए बुवाई के बाद एक से अधिक सिंचाई नहीं करनी चाहिए।
मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए निराई गुड़ाई प्रबंधन (Weeding hoe management for Lentil Cultivation)
बुवाई के 50 दिनों के अंदर मसूर(लेंटिल) में खरपतवार को नियंत्रित रखना अत्यंत आवश्यक होता है. दरअसल, यह फसल की बढ़वार में बाधा बनता है. मावठा गिरने के कारण मसूर(लेंटिल) की फसल में खरपतवार की अधिकता हो सकती है ऐसे में यदि फसल के दौरान मावठा गिर जाने में अच्छे से निराई-गुड़ाई करना चाहिए. ताकि खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकें.
मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए कीट नियंत्रण (Pest control for lentil cultivation)
वहीं मसूर(लेंटिल) में माहो, पत्ती छेदक और फली छेदक कीट का प्रकोप रहता है. माहो के नियंत्रण के लिए मोनोक्रोटोफॉस (15 एमएल मात्रा ) प्रति 1 मिली लीटर में घोल बनाकर छिड़काव करें. जबकि पत्ती और फली छेदक के लिए संशोधित कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए.
मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए कटाई (Harvesting of lentils)
मसूर(लेंटिल) की कटाई उस समय करें जब यह हरे से भूरे रंग की होने लगे. कटाई सुबह-सुबह उस समय करना चाहिए जब मौसम में नमी रहती है. इससे बीज कम झड़ता है और उत्पादन अच्छा होता है. बीज कटाई के बाद खलिहान में मसूर(लेंटिल) को अच्छी तरह सुखाने के बाद डंडों से पीटकर बीज को निकालना चाहिए.
मसूर(लेंटिल) की खेती के लिए उपज (Yield for lentil cultivation)
यदि अच्छी मसूर(लेंटिल) की अच्छी किस्म की बुवाई की जाती है तो सिंचित क्षेत्र में प्रति हेक्टयर 15 से 16 क्विंटल की उपज ली जा सकती है. वहीं असिंचित क्षेत्र से 8 से 10 क्विंटल की पैदावार होती है.
स्रोत कृषि-जागरण , MP कृषि ट्रेक्टर जंक्शन