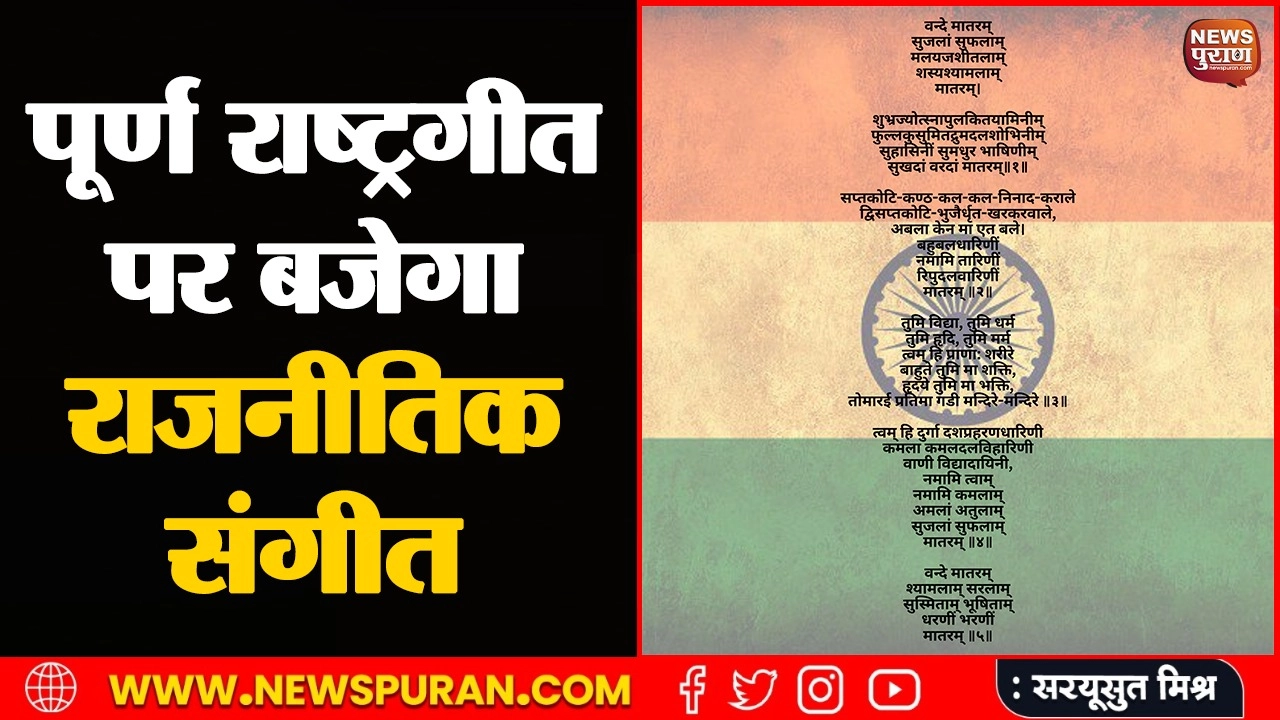गैर-कार्बनीकरण की दिशा में शुरू हुई प्रक्रिया
सार
योजना के अंतर्गत कुछ खास क्षेत्रों में कंपनियों के लिए हरित गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो इकाइयां निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। जो इकाइयां लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगी उन्हें बाजार से ये प्रमाणपत्र खरीदने होंगे..!

विस्तार
सरकार ने इस वर्ष जून में कार्बन क्रेडिट रेटिंग स्कीम (सीसीटीएस) की अधिसूचना जारी कर स्वागत योग्य कदम उठाया है। सरकार ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2021 के अंतर्गत यह पहल की है।
इस योजना के अंतर्गत कुछ खास क्षेत्रों में कंपनियों के लिए हरित गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो इकाइयां निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेंगी, उन्हें कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। जो इकाइयां लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगी उन्हें बाजार से ये प्रमाणपत्र खरीदने होंगे।
प्रत्येक कार्बन प्रमाणपत्र एक टन सीओ2ई (कार्बन डाईऑक्साइड समतुल्य) का होगा। इस योजना के माध्यम से देश में मूल्यों में पारदर्शिता वाला सुव्यवस्थित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का लक्ष्य है।भारत ने वर्ष 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) प्रतिबद्धता और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित किया है।
इस योजना के नियोजन, प्रशासन एवं नियमन में शामिल एजेंसियों एवं प्राधिकरणों में बिजली मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास निगरानी का दायित्व है। ऊर्जा क्षमता ब्यूरो (ईईबी) के पास योजना से जुड़े प्रशासनिक कार्य एवं कंपनियों के लिए लक्ष्य तय करने के अधिकार हैं।
भारतीय ग्रिड नियंत्रक को इन इकाइयों के पंजीकरण एवं उनके बीच होने वाले लेनदेन का लेखा-जोखा रखने से जुड़े दायित्व दिए गए हैं। केंद्रीय बिजली नियामकीय आयोग (सीईआरसी) को कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्र के नियमन से संबंधित अधिकार दिए गए हैं।
क्योटो संधि में 2008 से 2020 के बीच केवल अनुसूची-1 के देशों (विकसित देशों) के लिए उनके मात्रा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार उत्सर्जन लक्ष्य कम करना अनिवार्य किया गया था, जबिक अन्य देश भी उत्सर्जन कम करने पर सहमत हुए थे, मगर उनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।
परंतु 2015 में पेरिस में आयोजित 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) में स्थिति बदल गई। 2020 से क्योटो संधि की जगह लेने के लिए पेरिस में 21वीं सीओपी हुआ था। पेरिस समझौते में संबंधित देशों की क्षमताओं के आधार पर साझा मगर भिन्न उत्तरदायित्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था और केवल विकसित देशों के लिए कानूनी रूप से बाध्य लक्ष्यों पर ही ध्यान नहीं था।
वास्तव में आपसी सहमति के आधार पर एक ढांचा तय किया गया है, जिसमें सभी देश (विकासशील एवं विकसित) दोनों से अपेक्षा की गई है कि वे 2020 से प्रत्येक पांच वर्ष पर एनडीसी घोषित करें। देश अपनी प्रतिबद्धता में संशोधन कर इसे बढ़ा सकते हैं मगर इसमें कमी नहीं कर सकते हैं। पेरिस समझौता नाम लेना एवं शर्मिंदा करना (नेमिंग ऐंड शेमिंग) सिद्धांत पर आधारित है।
क्योटो संधि में अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन कारोबार परिभाषित किया गया था, जिसका इस्तेमाल कर विकसित देश (अनुसूची-1 के देश) अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते थे। यूरोपीय संघ (ईयू) और कुछ अन्य विकसित देशों में क्योटो संधि का अनुमोदन किए जाने के बाद उत्सर्जन व्यापार में तेजी आई मगर विकासशील देशों में इसे ठंडी प्रतिक्रिया मिली। हालांकि, भारत सहित इन देशों में कई परियोजनाएं स्वैच्छिक वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार में भाग ले रही हैं।
पेरिस समझौते के बाद अब बदली परिस्थितियों में जब प्रत्येक देश स्वयं अपनी जिम्मेदारी तय करने के लिए छोड़ दिए गए हैं, ऐसे में एनडीसी से जुड़े वादे पूरे करने के लिए एक ठीक ढंग से नियमित घरेलू उत्सर्जन कारोबारी ढांचे पर सभी देशों को विचार करना चाहिए। इस ढांचे में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का होना भी आवश्यक है।
सीसीटीएस को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। कार्बन क्रेडिट कारोबार बाजार आधारित ढांचा है, जिसकी जड़ें डिफरेंशियल मार्जिनल कॉस्ट की ठोस आर्थिक संकल्पना तक जाती हैं। विभिन्न इकाइयां उपने उत्पादों पर कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए डिफरेंशियल मार्जिनल कॉस्ट का सामना करती हैं। यह ढांचा उत्सर्जन घटाने वाली तकनीक, परियोजनाओं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर-कार्बनीकरण की दिशा में शुरू हुई प्रक्रियाओं में निवेश को बढ़ावा दे सकता है