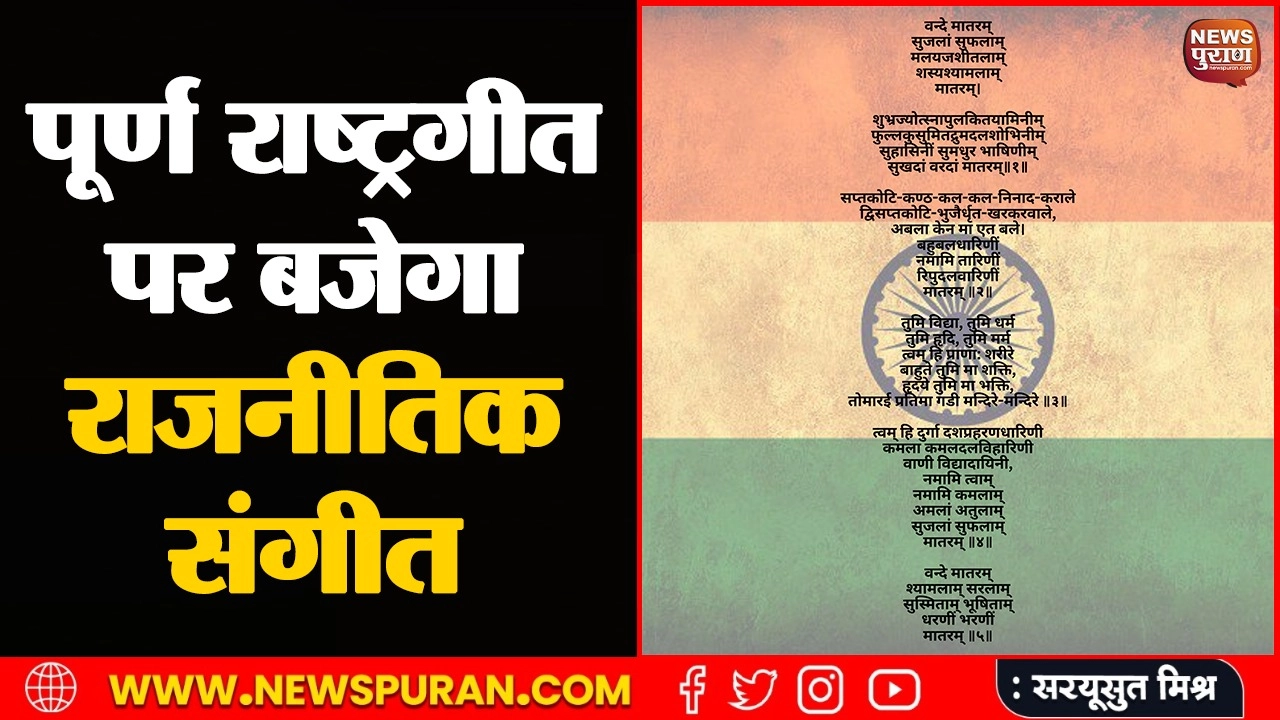पहाड़, खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं?
सार
उत्तरकाशी के जिस धराली गांव में बादल फटने और फिर तीव्र वेग के जल-प्रलय की आपदा आई है, ऐसी आपदाएं 1864, 2013 और 2014 में भी आ चुकी हैं..!!

विस्तार
‘प्रलय’ का नाम हमने सुना है, पर कभी कल्पना तक नहीं की। छायावाद के प्रणेता कवि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य ‘कामायनी’ जरूर पढ़ा है। उसमें प्रलय की विभीषिका के कई बिंब और एक अकेले मनुष्य का संघर्ष हमारे मानस पर अब भी अंकित है, लेकिन प्रलय के विनाश के मर्म तक हम पहुंच नहीं पाए। अलबत्ता एक कल्पना जरूर साकार होती गई।
हमारे कालखंड में उत्तरकाशी के महाभूकंप और 2013 के केदारनाथ मंदिर क्षेत्र के प्रलय का साक्षी बनने का मौका जरूर मिला है और वह भी टीवी चैनलों के जरिए। उत्तरकाशी के जिस धराली गांव में बादल फटने और फिर तीव्र वेग के जल-प्रलय की आपदा आई है, ऐसी आपदाएं 1864, 2013 और 2014 में भी आ चुकी हैं।
आखिर पहाड़ इतने खौफनाक और खतरनाक क्यों होते जा रहे हैं? क्या पहाड़ में आवास दूभर हो गया है? लगातार भू-स्खलन और बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्या हिमालय पर्वत के हिस्से भी दरकने और बड़े-बड़े पत्थरों के रूप में गिरने लगे हैं? इन घटनाओं और आपदाओं में बारिश और बादल फटने की घटनाएं ‘कुदरत का कहर’ मानी जा सकती हैं।
इसके अलावा घर, दुकान, मंदिर, इमारतें, होटल आदि का जमींदोज होना, नतीजतन मौत के आंकड़े बढ़ते रहने की आपदाएं ‘मानव-निर्मित’ हैं। यह हमारा नहीं, मौसम और भूगर्भ वैज्ञानिकों का विश्लेषण है। विकास के नाम पर पहाड़ खोदे जा रहे हैं। पहाड़ों को चीरकर सुरंगें बनाई जा रही हैं। रेल की पटरी बिछाई जा रही है। नदी-नालों के किनारे अथवा उन्हीं के भीतर होटल, रिजॉर्ट की बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं।
उत्तराखंड में ही जिस 50,000 वर्ग हेक्टेयर में जंगलात थे, अब वहां पक्की इमारतें चिन दी गई हैं। मौजूदा उत्तरकाशी के प्रलय में धराली गांव ही बह कर मिट्टी-मलबा हो गया। राज्य के मुख्य सचिव आनंदवर्धन के मुताबिक, धराली गंगोत्री के रास्ते में मुख्य ठहराव स्थल है। आबादी मात्र 700 के करीब है।इनमें से 100 लोग लापता हैं। 150 घरों से ज्यादा वाले गांव में 50 से ज्यादा घर, 30 से ज्यादा होटल-रिजॉर्ट, करीब 25 होम स्टे तबाह हो चुके हैं। जो मंजर सामने आया है, वह प्रलय नहीं तो क्या है?
2013 का केदारनाथ मंदिर वाला प्रलय इतना विनाशकारी था कि 6000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब प्रलय को इतना विध्वंसक नहीं माना जा रहा है, लेकिन मौत के अधिकृत आंकड़े अभी सामने आने हैं। गौरतलब यह भी है कि मौजूदा प्रलय से पहले भूस्खलन का औसत 250 था, जो 2023 तक 1600 से अधिक हो गया।
इतना गुना भूस्खलन क्यों और कैसे बढ़े? पहाड़ इतनी मात्रा में क्यों टूटने लगे हैं? इस सवाल का जवाब न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने दिया है। कुछ उच्चाधिकार प्राप्त समितियां जरूर बनाई जाती रही हैं, लेकिन वे विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के सुझावों को नकारती रही हैं। मसलन-वैज्ञानिकों के सवाल हैं कि पहाड़ों में ‘फोरलेन सडक़’ बनाना क्यों जरूरी है? दो लेन की सडक़ें पर्याप्त और सहज हैं।
ऐसे निर्माण दिखावटी विकास तो हैं, लेकिन विनाश और मौत के अंधे कुएं भी तैयार कर रहे हैं। केदारनाथ प्रलय के बाद रडार लगाने की बात सामने आई थी, ताकि बादल फटने और जल-प्रलय के पूर्व संकेत मिल सकें। उनका क्या हुआ? उत्तरकाशी प्रलय के कुछ भी संकेत क्यों नहीं मिल सके। मात्र 34 सेकंड में बहुत कुछ मलबा हो गया। हिमालयी क्षेत्र के लिए ‘ग्लोबल वार्मिंग’ और ‘जलवायु परिवर्तन’ भी खतरनाक स्थितियां हैं। उनसे एक अलग स्तर पर लडऩे की जरूरत है।
आपदा के लिहाज से धराली ‘टाइम बम’ पर बैठा माना जाता रहा है, लेकिन इसे कहीं और शिफ्ट नहीं किया गया। वरिष्ठ भूगर्भ वैज्ञानिक प्रो. एसपी सती का कहना है कि धराली ट्रांस हिमालय (4000 मीटर से ऊपर) में मौजूद मेन सेंट्रल थस्र्ट है। यह एक दरार होती है, जो मुख्य हिमालय को ट्रांस हिमालय से जोड़ती है। यह भूकंप का अति संवेदनशील क्षेत्र भी है। इस खतरे को समझना होगा।