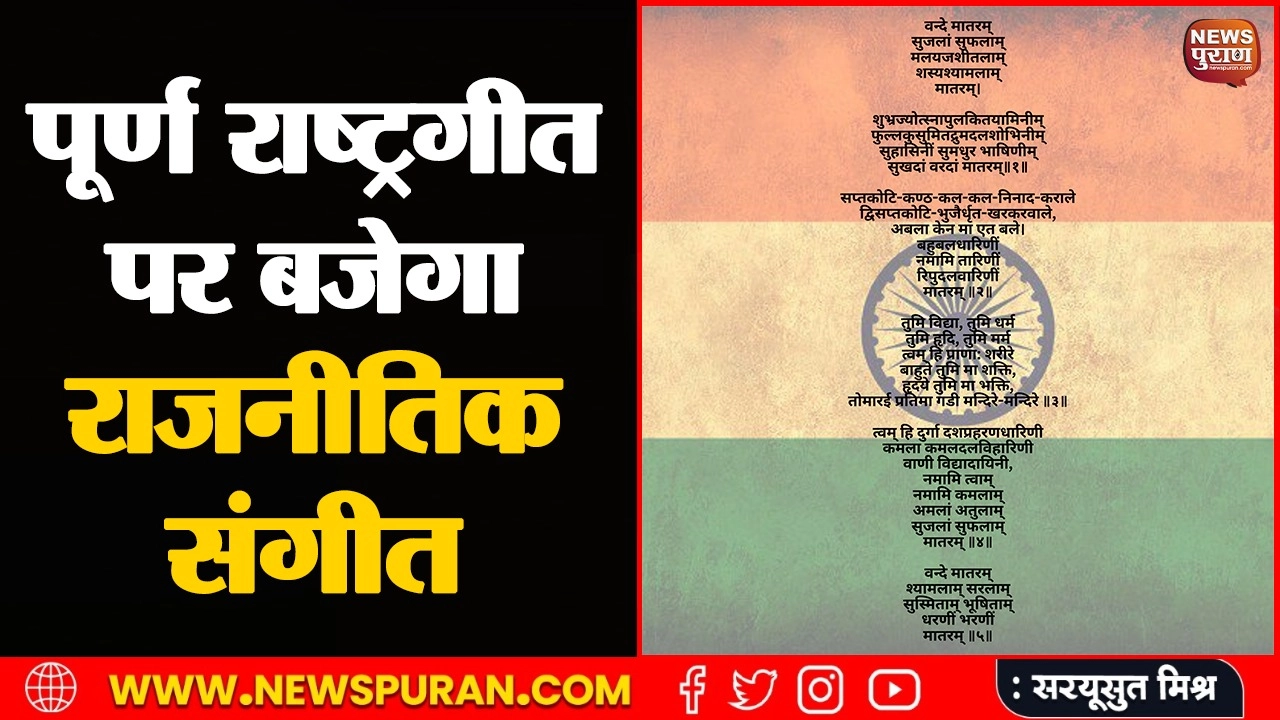बिक रहे हैं, मूल्य और स्वप्न
सार
वैश्विकता, बाजारवाद, उत्तर पूंजीवाद, अंध साम्राज्यवाद, अंध राष्ट्रवाद पर संगोष्ठी-सेमिनार चल रहे हैं, इस त्रासद समय में कविता-कथा में नयी उम्मीद जगाने वाला नवलेखन है। स्थापित लेखकों को भ्रम है कि युवा लेखकों का बचपन छीन लिया गया है और वे असमय परिपक्वता के शिकार हैं..!!

विस्तार
इन दिनों हम अंधेरे दु:स्वप्न सरीखे त्रासद समय में हैं, धर्मान्ध ताकतों के लिए शाइनिंग इंडिया, शॉपिंग मॉल, मेगा ट्रेड फेयर की चहल-पहल है, हॉलीवुड-बॉलीवुड की अश्लीलताएं हैं, तांत्रिकों की बलि पूजा है, दूसरी ओर किसानों की आत्महत्याएं हैं। वैश्विकता, बाजारवाद, उत्तर पूंजीवाद, अंध साम्राज्यवाद, अंध राष्ट्रवाद पर संगोष्ठी-सेमिनार चल रहे हैं। इस त्रासद समय में कविता-कथा में नयी उम्मीद जगाने वाला नवलेखन है। स्थापित लेखकों को भ्रम है कि युवा लेखकों का बचपन छीन लिया गया है और वे असमय परिपक्वता के शिकार हैं। युवा लेखक अपनी हताशा को भी देख रहे हैं और अंधेरे समय को भी। उन्हें पता है, क्रांति यकायक नहीं आएगी। जहां आज के साहित्य में प्रयोग की निजता पर बल है, वहीं सामाजिक सरोकार भी बेचैन करने वाला है।
सर्वग्रासी राजनीति के चलते पक्षधरता या प्रतिबद्धता गायब है। सब कुछ ग्लोबल है और जहां सुपर पावर अमरीका का आतंक है, गरीबी का ग्राफ ऊपर है। उत्तर आधुनिकता के विमर्शकार मान रहे हैं कि इतिहास का अंत हो गया है, विचारधारा का अंत हो गया है। सब कुछ ब्रांड है, बिक रहा है, मूल्य और स्वप्न। उत्तर आधुनिकता दुहरी यंत्रणा है। न हम ठीक से आधुनिक हो पा रहे हैं, न ग्लोबल। साम्राज्यवाद की दासता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। उत्तर पूंजीवाद के घपले हमें भटकते हुए सन्नाटे में ले जा रहे हैं। साहित्य में विचार और दर्शन की भूमिका को नगण्य मानने वाले विद्वान आज भी बहुतायत हैं। साहित्यिक बिरादरी का यह वर्ग साहित्यिक अभिव्यक्ति में विचार और दर्शन की उपस्थिति को न केवल अनावश्यक मानता है, बल्कि विचार व दर्शन की चाशनी को देखने मात्र से इनकी भौंहें तिरछी होने लगती हैं।
विचारधारा का अंत, इतिहास का अंत जैसी अवधारणाओं को गढ़ कर वे साहित्य को जीवन से परे भाववाद की भूलभुलैया में ले जाते हैं। यहां यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि आधुनिक काल में जब-जब हमारे साहित्य को जीवन के यथार्थ से, जनता की मुक्ति और उसके सांस्कृतिक उत्थान के संघर्ष से विमुख करने के प्रयत्न हुए हैं, तब-तब निशाना प्रेमचंद को बनाया गया है। जबकि प्रेमचंद की महानता का स्रोत यह है कि अपने उन सैद्धान्तिक रुझानों और वैचारिक पूर्वाग्रहों से जो उन्हें अपने युगीन समाज से विरासत में मिले थे, वे निरंतर जूझते रहे।
फलस्वरूप उनकी संवेदना भारतीय समाज के मूल अंतर्विरोधों को सामने लाने में सफल हुई। प्रेमचंद भारत के किसान को सुखी देखना चाहते थे। भारत का वह किसान वस्तुस्थिति से निराश और हताश आज आत्महत्या करने को विवश है। प्रेमचंद स्त्री की मुक्ति चाहते थे। स्त्री-समाज आज भी असुरक्षित अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है। वे बलात्कारियों की हवस का शिकार हो रही हैं, मुक्ति की बात तो कोसों दूर, महानगरों, नगरों, कस्बों, गांवों और दूरदराज के अंचलों में घरों की सीलन भरी कोठरियों में गीली लकड़ी की तरह सुलग और घुट रही हैं। पुरुष वर्चस्व का शिकंजा उनकी गर्दनों पर पहले जैसा ही कसा हुआ है।
दलित समाज आजादी के इतने वर्षों के बाद आज भी दमन और उत्पीडऩ का शिकार है, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष कर रहा है। आज सांप्रदायिक धर्मोन्माद इतने चरम रूप में है कि पूजा-उपासना के ध्वंस की बात अलग, सांप्रदायिक जुनून के चलते निरंतर हत्याएं हो रही हैं। गोरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को भी इसी प्रसंग में देखा जाना चाहिए। आज तो पहले का पूंजीवाद सांस्थानिक पूंजीवाद में रूपांतरित होकर, कमजोर, पिछड़े हुए और विकासशील देशों को अपने कर्ज के लपेटे में लेकर, उन्हें अपने बाजार के रूप में बदलता हुआ, आश्वस्त और निश्चिंत, उनका आर्थिक दोहन कर रहा है।
यह हमारा समय है, यहां पाने और न पाने के बीच द्वंद्व सबसे अधिक मुखर है। लोग या तो बाजार की चकाचैंध को अचकचाए खड़े निहार रहे हैं या फिर भौतिक संसाधनों से भरे अपने घर में कैद होकर निरंतर अकेले और असहाय होते जा रहे हैं। हम भारतीय अपनी सामाजिकता के लिए जितने अधिक जाने जाते हैं, उस पर इतना घनघोर किस्म का संकट इसके पूर्व कभी नहीं आया। लेखक का दायित्व सबसे गुरुत्तर हो जाता है। जब एक लेखक को इन भौतिक संसाधनों के मकडज़ाल से बचकर गलियों और सडक़ों की धूल छाननी होगी।