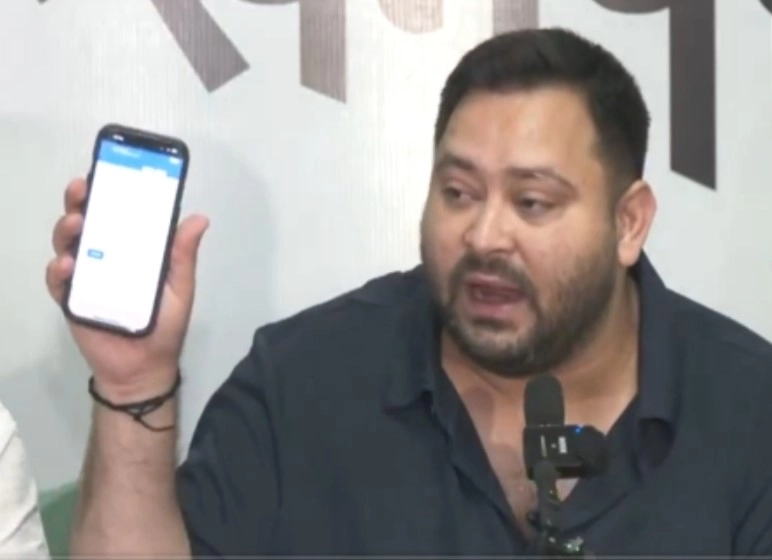आम धारणा है कि बंदर हमारे पूर्वज थे, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे और बंदरों के पूर्वज किसी समय में एक ज़रूर थे, लेकिन इंसान और बंदर का विकास अलग अलग रास्ते पर हुआ, इसीलिए हम इंसान बने और वे बंदर। इस नाते बंदर रिश्ते में हमारे पूर्वज नहीं, बल्कि हमारे कजिन हुए। इसे समझने के लिए क्रमिक विकास पर कुछ बुनियादी बातें जानना ज़रूरी है। क्रमिक विकास जीव जंतुओं और वनस्पतियों में पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले अनुवांशिक लक्षणों में होने वाले चिरायु परिवर्तन को कहते हैं। यह प्रक्रिया जैविक संगठन के हर स्तर (प्रजाति, जीव विशेष या कोशिका) के स्तर पर बढ़ती विविधता के लिए ज़िम्मेदार है। विकासवाद की धारणा है कि समय के साथ जीवों में क्रमिक-परिवर्तन होते हैं। इस सिद्धान्त के विकास का लम्बा इतिहास है। 18वीं सदी तक पश्चिमी जीवविज्ञानी चिन्तन में यह विश्वास जड़ जमाये था कि प्रत्येक जीव में कुछ ऐसे विलक्षण गुण होते हैं जो बदले नहीं जा सकते। इस वैचारिक धारा को essentialism कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में यह धारणा बदलने लगी।
19वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी जीवविज्ञानी ज्याँ बैप्टिस्ट लैमार्क ने अपना विकासवाद का सिद्धान्त दिया। लैमार्क का सिद्धांत क्रम-विकास (evolution) से सम्बन्धित प्रथम पूर्णत: निर्मित वैज्ञानिक सिद्धान्त था। लैमार्क का सिद्धांत था कि वातावरण के परिवर्तन के कारण ही जीव की उत्पत्ति, अंगों का व्यवहार या अव्यवहार व जीवनकाल में अर्जित गुणों का जीवों द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। लैमार्क ने इसके उदाहरण के रूप में जिराफ़ का जिक्र किया, और कहा कि जिराफ़ कभी छोटी गर्दन वाला गधा-नुमा जीव रहा होगा, जिसके आसपास की घास खतम हो जाने की वजह से उसे ऊँचे पेड़ों की पत्तियाँ खाने हेतु गर्दन ऊँची करनी पड़ती होगी, और इसी प्रक्रिया में कई पीढ़ियों के विकास के बाद वह जिराफ़ बन गया। हालाँकि बाद में लैमार्क का यह सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ, लेकिन उस दौर में यह सिद्धांत भी एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जिसने essentialism की जड़ व पुरातन वैचारिक धारा पर जीव विज्ञान के इतिहास में पहली बार गहरी चोट की थी। इसके बाद आए डार्विन, जिन्होंने प्रसिद्ध जहाज़ "एच एम एस बीगल" पर यात्रा करते हुए, प्रशांत महासागर के इक्वेटर पर स्थित गैलापागोस द्वीपसमूह पर जीव जंतुओं, पक्षियों, उनकी चोंच के प्रकार, पंजे के प्रकार आदि का लंबा और गहन अध्ययन करते हुए अपने अवलोकनों के आधार पर कुछ ऐसी प्रस्थापनाएँ दी जिसने क्रमिक विकास विज्ञान की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। वह था प्राकृतिक चयन (Natural Selection) का सिद्धांत। जिस प्रक्रिया द्वारा किसी प्रजाति में कोई जैविक गुण कम या अधिक हो जाता है उसे 'प्राकृतिक चयन' कहते हैं। यह एक धीमी गति से क्रमशः होने वाली non random प्रक्रिया है। प्राकृतिक चयन ही क्रमिक-विकास की प्रमुख कार्यविधि है। डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक-विकास के सिद्धांत को अपनी किताब "जीवजाति का उद्भव" (Origin of Species) में 1859 में प्रकाशित किया।
प्राकृतिक चयन द्वारा क्रमिक विकास की प्रक्रिया को निम्नलिखित अवलोकनों से द्वारा साबित किया जा सकता है: 1. जितनी संतानें संभवतः जीवित रह सकती हैं, उस से अधिक पैदा होती हैं 2. आबादी में रूपात्मक, शारीरिक व व्यवहारिक लक्षणों में विविधता होती है 3. विभिन्न लक्षण उत्तरजीविता (survival) और प्रजनन (reproduction) की अलग अलग संभावना प्रदान करते हैं 4. इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है।
प्राकृतिक चयन का अर्थ उन गुणों से है जो किसी प्रजाति को बचे रहने और प्रजनन करने में सहायता करते हैं और इसकी आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है। यह इस तथ्य को और तर्कसंगत बनाता है कि इन लक्षणों के धारकों की सन्ताने अधिक होती हैं और वे यह गुण वंशानुगत रूप से भी ले सकती हैं। डार्विन ने यह सिद्धांत तब प्रस्थापित किये जब जेनेटिक्स के अध्ययन के लिए न तो कोई तकनीक उपलब्ध थी, न ही डीएनए की खोज हुई थी, न ही सूक्ष्मजीवियों के विषय में जानने के लिए उस दौर में पर्याप्त यंत्र उपलब्ध थे। इलेक्ट्रान माइक्रोस्कोप के आविष्कार, डीएनए व जेनेटिक कोडॉन की खोज, व molecular genetics के विकास ने डार्विन के सिद्धांतों की नींव पर ही क्रमिक विकास के विषय में हमारे ज्ञान का कई गुना विस्तार किया। जेनेटिक्स के विकास और सूक्ष्मजीवियों के और गहन अध्ययन के बाद पता चला कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया उत्तरजीविता और प्रजनन की आभासी उद्देश्यपूर्णता से उन लक्षणों को बनाती और बरकरार रखती है जो अपनी कार्यात्मक भूमिका के अनुकूल हों। अनुकूलन का प्राकृतिक चयन क्रम-विकास का एक कारण ज़रूर है, लेकिन क्रम-विकास के और भी ज्ञात कारण हैं। माइक्रो-क्रम-विकास के अन्य गैर-अनुकूली कारण उत्परिवर्तन(mutation) और genetic drift हैं। खैर वापस आते हैं बंदर और इंसान के रिश्ते पर। तो हमारे साझे पूर्वज संभवतः जंगल के पेड़ों पर ही रहा करते होंगे, और माँसाहारी पशुओं के खतरे से दूर पेड़ की ऊंचाइयों पर उछलते कूदते जंगल के फल फूल आदि पर मज़े से जीते रहे होंगे। किन्हीं कारणवश, किसी भयंकर दीर्घकालिक सुखाड़ या जंगल की आग, या किसी तीव्र दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन ने उनके इलाके के जंगलों का नाश कर दिया होगा, और इस प्रकार उन्हें पेड़ से उतरकर मैदानों और grasslands में भोजन पानी की खोज में आने को मजबूर किया होगा, यूँ कहिए, धकेला होगा। तब पहली बार हमारे पूर्वजों में से कुछ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू हुई होगी। मैदानों और झाड़ियों में माँसाहारी नरभक्षी जानवरों, शेर, बाघ, चीतों का भी खतरा रहा होगा, जिसने हमारे पूर्वजों में से कुछ को दो पैरों पर खड़ा होकर दुश्मन का खतरा दूर से भाँप लेने का advantage दिया होगा। दोनों हाथ फ्री हुए तो हमारे पूर्वजों को नुकीले पत्थरों व लकड़ियों के हथियार बनाना सिखाया होगा, और इस क्रम में हथेली की उंगलियों की सूक्ष्म पकड़ व fine motor skills विकसित की होगी। इसके साथ ही प्रकृति के साथ संघर्ष की इस प्रक्रिया में, मनुष्य ने शिकार करना सीखा होगा और माँसाहार की शुरुआत हुई होगी। माँसाहारी प्रोटीन से भरपूर भोजन से पोषित उनके मष्तिष्क का और तेज़ी से विकसित हुआ होगा। ज़ाहिर है हमारे सभी पूर्वज इस विकास की दिशा को पकड़ने में असफल रहे होंगे और प्रकृति ने ऐसे अनुकूल विकास का चयन करते हुए बाकियों को छाँट दिया होगा। हमारे सबसे करीबी भाई, और शारीरिक रूप से हमसे कहीं बलशाली, निएंडरथल इसी प्रक्रिया में खतम हो गए, प्रकृति द्वारा छाँट दिए गए।
By : - Shravan Yadav