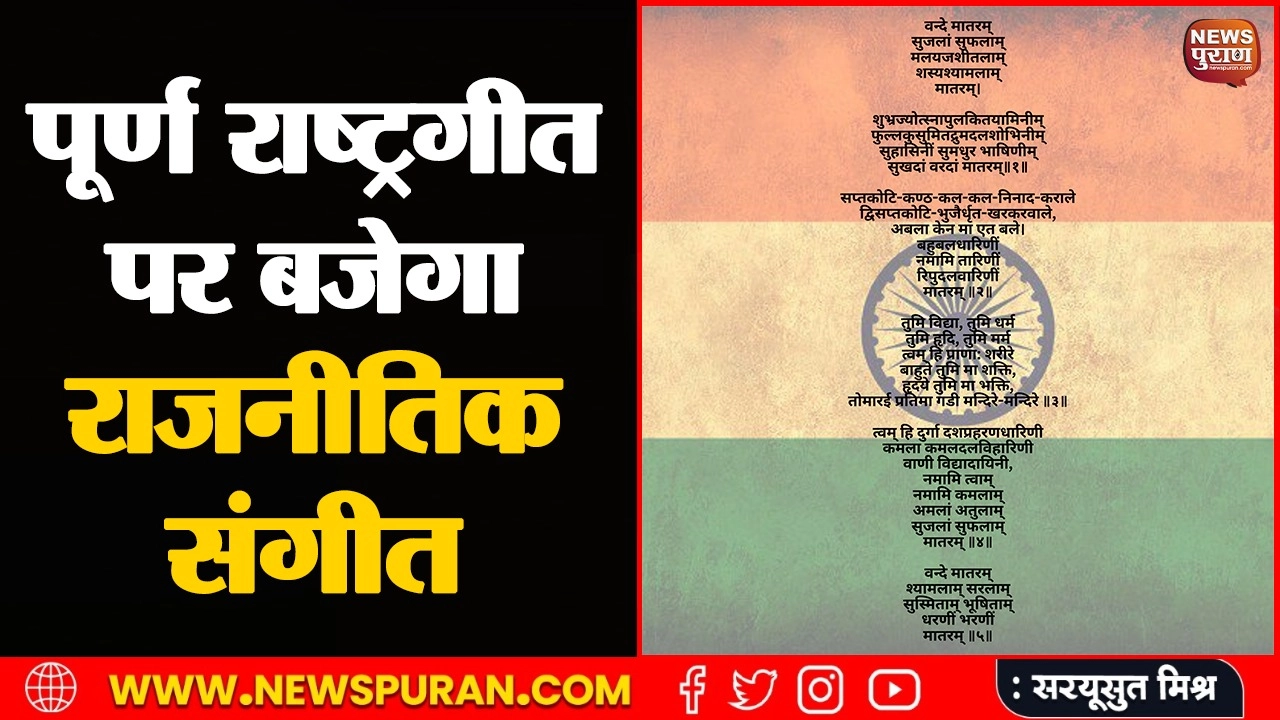शहरी सामूहिकता
सार
जब कंपनियां, कर्मचारी और योजनाकार सब एक जगह होते हैं, तो वे साझा बुनियादी ढांचे, संयुक्त श्रम और नवाचार का लाभ उठाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल से लेकर एडवर्ड ग्लेसर तक तमाम अर्थशास्त्रियों ने एक ही जगह उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले ऐसे केंद्रों की सराहना करते हुए इन्हें उत्पादकता एवं विकास का इंजन बताया है..!!
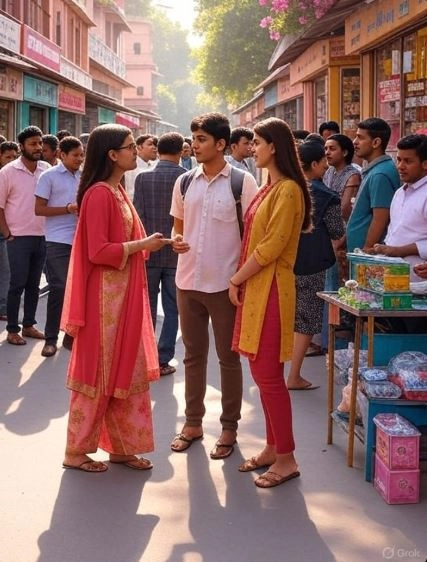
विस्तार
शहरी अर्थव्यवस्थाओं में सामूहिकता बहुत मायने रखती है। जब कंपनियां, कर्मचारी और योजनाकार सब एक जगह होते हैं, तो वे साझा बुनियादी ढांचे, संयुक्त श्रम और नवाचार का लाभ उठाते हैं। अल्फ्रेड मार्शल से लेकर एडवर्ड ग्लेसर तक तमाम अर्थशास्त्रियों ने एक ही जगह उपलब्ध सभी सुविधाओं वाले ऐसे केंद्रों की सराहना करते हुए इन्हें उत्पादकता एवं विकास का इंजन बताया है। पिछले कुछ समय से भारत के कई बड़े शहरों ने अपने यहां ऐसी ही एकीकृत सुविधाओं, रोजगार ढांचे को विकसित करने पर जोर दिया है।
बेंगलूरु ने तकनीकी कंपनियों और इंजीनियरों को आकर्षित किया है, तो मुंबई ने अपने कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में ही वित्त, मीडिया और महत्त्वाकांक्षी लोगों को केंद्रित किया है। इसी तरह दिल्ली ने भी राजनीति, अफसरशाही और इन सबके बीच रहन-सहन को आसान बनाने वाली हर चीज को एक साथ लाकर विकास का अनूठा गुलदस्ता बनाया है।
सैद्धांतिक रूप में एकीकृत शहरी व्यवस्था से उत्पादकता में वृद्धि होनी चाहिए थी और शायद कुछ समय के लिए ऐसा हुआ भी। लेकिन अब जबकि बेंगलूरु अत्यधिक यातायात के दबाव से जूझ रहा है, मुंबई में आवासीय संकट है और दिल्ली का दम धुएं (प्रदूषण) से घुट रहा है, तो सवाल उठता है कि विकास का यह रास्ता कितना कारगर है? देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शहरों का योगदान 60 फीसदी से अधिक है और वर्ष 2030 तक इसके बढ़कर 70 फीसदी तक हो जाने का अनुमान है। दिल्ली, बेंगलूरु और मुंबई जैसे महानगरों में लगातार पूंजी निवेश हो रहा है और श्रमबल खिंचा चला रहा है। सरकार भी स्मार्ट सिटी, स्वच्छ ऊर्जा और हाई-स्पीड रेल जैसी सुविधाओं के साथ इन शहरों की गतिशीलता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।
इनसे शहरी जीवन आसान जरूर लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि बेंगलूरु की दिनचर्या हर रोज 190 किलोमीटर के दायरे में घूमती है। कर्नाटक में इंस्टीट्यूट फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक चेंज के अनुमान के मुताबिक यातायात जाम के कारण बेंगलूरु को अपने उत्पादक घंटों में कमी आने की वजह से 1,170 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। मेट्रो अभी पूरे शहर और इसके आसपास उभरते उपनगरों को कवर नहीं कर पाई है। कागजों में देश के रहने लायक सबसे अच्छे शहरों में शुमार पुणे ने पिछले एक दशक में अपनी हरियाली का एक तिहाई हिस्सा खो दिया है। भुवनेश्वर और नागपुर लगातार बढ़ती गर्मी से परेशान हैं। इस वजह से इन दोनों शहरों में पहले ही अनौपचारिक कामगारों की उत्पादकता 10 से 13 फीसदी तक कम हो गई है।
असल बात यह है कि समूहीकरण केवल शहरों में अधिक से अधिक लोगों के बसने का नाम नहीं है। यह जीवन की गुणवत्ता के बारे में है। शहरी उत्पादकता तब बढ़ती है जब लोग आपस में सहयोग करते हैं। एक साथ घूमते-फिरते हैं और एक-दूसरे से सीखते हैं। लेकिन यदि शहर में काम के सिलसिले में हर रोज दो घंटे सफर करना पड़े, आवास पर ही आधी कमाई खर्च हो जाए और लू चलने से लोगों की रोज की कमाई पर ही संकट आ जाए तो सुविधाओं का केंद्रीकरण बेमानी हो जाता है।
नगर निकायों के कामकाज पर 2024 में किए गए एक शोध में पता चलता है कि एकीकृत विकास के लिए शहरों में कितनी कम या खराब सुविधाएं हैं। इस अध्ययन में शामिल152 नगर पालिकाओं में से केवल 94 के पास ही अपनी विकास योजनाओं से संबंधित डेटा मिला। इनमें भी सिर्फ 59 ने अपने डेटा को जीआईएस यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली के आधार पर अपडेट किया था। अध्ययन का हिस्सा रहे कुल शहरी निकायों में से केवल 37 के पास एक सक्रिय गतिशील योजना पाई गई और केवल 16 निकाय ही नगर नियोजन योजना के अंतर्गत कामकाज के पैमाने पर खरे उतरे। कुल 113 नगर पालिकाओं के पास ही योग्यता प्राप्त योजनाकार हैं। खंडित और असंगत योजना ढांचे के कारण शहरों की वह व्यवस्था कमजोर होती है जो व्यापक आबादी को अराजक के बजाय उत्पादक बनाने में मदद करती है।
देश अभी आंशिक सामूहीकरण प्रक्रिया से गुजर रहा है जहां कंपनियां और कुशल श्रमबल तो आ रहे हैं लेकिन वे कमजोर बुनियादी ढांचे और पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपनी आबादी को उत्पादक बनाने के लिए शहरों को अपनी क्षमताओं को समझना होगा। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के हालिया निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि जनसंख्या और उसके घनत्व के हिसाब से वेतन लचीलापन या प्रत्यास्थता भारतीय शहरों में 1 से 2 फीसदी ही है। यह अधिक विकसित देशों की शहरी अर्थव्यवस्थाओं के 4 से 6 फीसदी से काफी कम है। वेतन के लचीलेपन में यह अंतर न केवल शहरी बुनियादी ढांचे की कमी, बल्कि समन्वित एवं भविष्योन्मुख रणनीतिक योजनाओं के गंभीर अभाव को भी दर्शाता है।
शहरों को ऐसी मजबूत डेटा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो अपनी सेवाओं से लेकर भू-उपयोग योजनाओं तक आम आदमी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तत्काल निर्णय लेने में मददगार साबित हो। नियोजन प्रक्रियाओं को लचीला होना चाहिए जिससे जनसांख्यिकीय बदलावों, जलवायु जोखिमों और आर्थिक स्थिति परिवर्तन का पूर्वानुमान आसानी से लग सके। शहरों के विखंडित प्रशासन को दुरुस्त करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। कई शहरों में आवास, परिवहन और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में क्षेत्राधिकार सीमाओं की गड़बड़ी के कारण समन्वित योजनाएं बनाने में दिक्कत पेश आती है। शहरों के विकास की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे श्रम गतिशीलता को बल मिले और आर्थिक समावेश बढ़े। इससे यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लोग न केवल शहरों में रहें, बल्कि वे सुविधाजनक आवाजाही करें और सार्थक रूप से नौकरियों, सेवाओं एवं नवाचार नेटवर्क से भी जुड़ें।
एशिया के अन्य शहरों में सिंगापुर का ही उदाहरण लें, जहां एकीकृत भू-उपयोग और परिवहन योजनाएं इस तरह डिजाइन की गई हैं कि लोगों की उत्पादकता बढ़ गई है और वे यहां रहने के लिए प्रेरित होते हैं। वहां के मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (रेल प्रणाली) से प्रतिदिन 30 लाख से अधिक लोग आवाजाही करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है, क्योंकि वहां बहुत पहले ही भीड़भाड़ से निपटने के लिए ठोस योजनाएं तैयार कर ली गई थीं।
इसी तरह वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर ने भी अपनी बढ़ती आबादी के मुद्दों से निपटने के बेहतर इंतजाम किए हैं। यहां केंद्रित औद्योगिक क्षेत्र और रणनीतिक ढांचागत निवेश के कारण श्रम उत्पादकता हनोई शहर की तुलना में लगभग दोगुनी है। ये इस बात के जीते-जागते उदाहरण हैं कि कोई शहर अपनी आबादी से कैसे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हासिल कर सकता है।
आज अधिकांश भारतीय शहर पलायन के दौर से गुजर रहे हैं। यह इसलिए नहीं हो रहा कि वे सफलताओं की सीमाओं को पार कर चुके हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अभी तक अपने निवासियों एवं उद्योगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े वादे तक पूरे नहीं किए हैं। आबादी, नौकरियों और सेवाओं को एक जगह लाने से उत्पादकता एवं नवाचार को बढ़ाने तथा आर्थिक मौकों को भुनाने की उम्मीद थी लेकिन समन्वित रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। नतीजतन कई शहरों की आबादी तो बढ़ी है, लेकिन उनकी गतिशीलता और उत्पादकता नहीं बढ़ी है। तरक्की के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। भारतीय शहरों को अपने पुनर्संयोजन की प्रक्रिया अपनानी होगी। दीर्घावधि विकास को ध्यान में रखते हुए उन्हें नए सिरे से गुणवत्ता, लचीलेपन और समानता पर केंद्रित एवं बेहद सुविचारित योजनाएं लागू करनी होंगी।