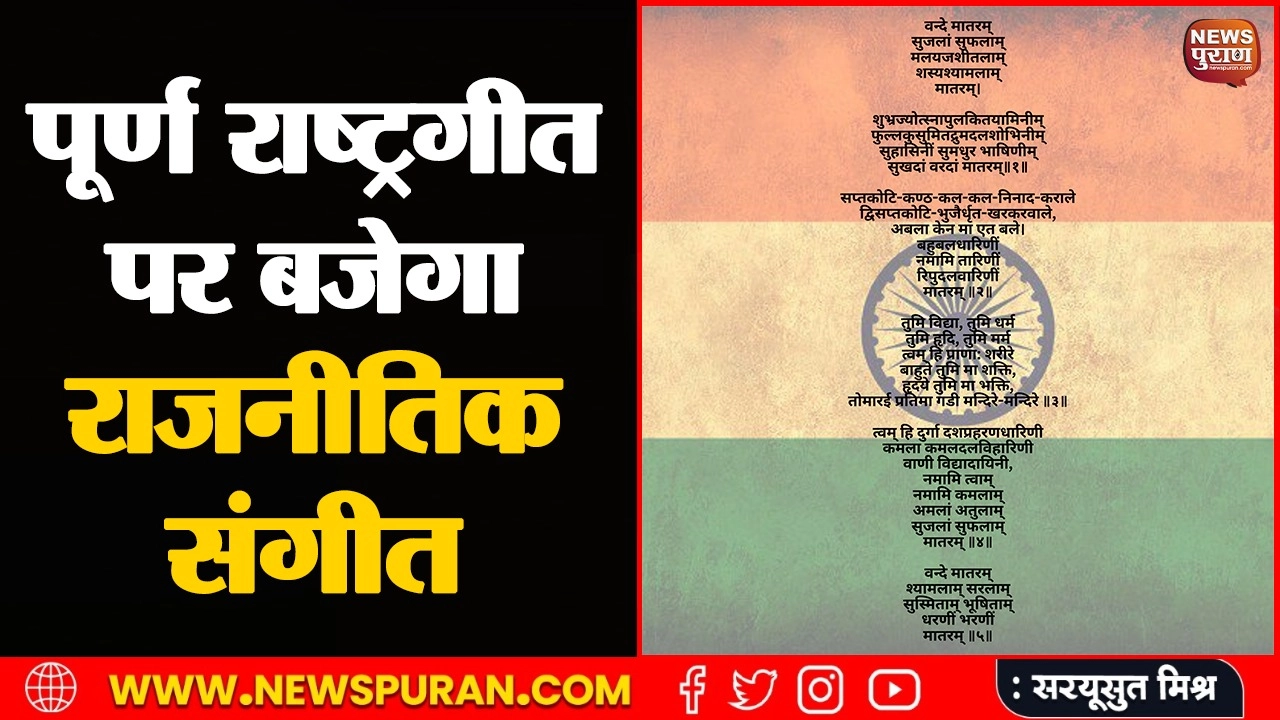सुप्रीम कोर्ट का संकेत संसद हो सचेत
सार
मानहानि का अपराध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का घात प्रतिघात राजनीति और मीडिया के विरोध में एक अस्त्र के रूप में उपयोग होता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मानहानि का अपराध बाधक बनता है..!!

विस्तार
कई बार तो ऐसा लगता है, इस कानूनी प्रावधान का दुरुपयोग हो रहा है. इसका उपयोग राजनीति में सर्वाधिक देखा जाता है. पत्रकारिता भी इससे प्रभावित होती है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मानहानि के मामले में सुनवाई के दौरान की गई एक टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, कि अब समय आ गया है, कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से हटाया जाए. मानहानि के मामले सिविल प्रकरणों में भी चलते हैं. इसे अपराध की श्रेणी में रखे जाने से ऐसे मामलों में सजा का प्रावधान होता है.
अनेक मामलों में ऐसा देखा गया है मानहानि के अपराध में कानून का दुरुपयोग कर फंसाया जाता है. पत्रकारिता के बड़े-बड़े संस्थानों में तो मानहानि के आपराधिक मामले चलते ही रहते हैं.
प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण है, किसी भी नागरिक की गरिमा के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकारों में यह भी शामिल है. सिविल प्रकरणों में मानहानि के केस तो स्वीकार हो सकते हैं, लेकिन इसको अपराध की श्रेणी में रखकर सजा जैसे प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात पहुंचाते हैं.
सबसे लेटेस्ट मामला राहुल गांधी का है. मोदी समाज के मानहानि के लिए उन पर आपराधिक मुकदमा चलाया गया था. उन्हें उन्हें 2 साल की सजा हुई. इस कारण उनकी संसद सदस्यता समाप्त हो गई थी. उच्च अदालत द्वारा सजा पर रोक लगाए जाने के बाद फिर से उनकी सदस्यता बहाल हुई थी. इस पर राजनीति भी खूब हुई. कांग्रेस द्वारा यहां तक आरोप लगाया गया कि बीजेपी की सरकार द्वारा जानबूझकर मानहानि के आपराधिक मामले में राहुल गांधी को फंसाया गया है.
यहां तक कि अदालत के निर्णय पर भी सवाल उठाए गए थे. अगर मानहानि अपराध की श्रेणी में नहीं होता तो फिर राहुल गांधी को सजा नहीं हो सकती थी. उनकी किसी बात से अगर किसी को ठेस पहुंचती तो वहां सिविल केस के रूप में अदालत में जा सकता है.
मानहानि को अपराध की श्रेणी में 1800 के दशक में ब्रिटिश राज द्वारा लाया गया था. अंग्रेजों को भारत के लोगों पर शासन करना था. उन पर दबाव और डर बनाए रखना था. उनके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठे इसी नजरिए से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए इसे अपराध के रूप में लाने के लिए कानून बनाया गया था.
सदियों बाद भी क्या वही मानसिकता काम करेगी. सूचना क्रांति के इस दौर में भी असहमति को दबाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आधात पहुंचाने के इस कानून को जारी रखना कहां तक जायज है.
सुप्रीम कोर्ट के सामने मानहानि को अपराध से बाहर करने का विषय एक दशक पहले भी आया था. कई प्रमुख राजनेताओं ने अदालत में केस लगाया था. वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान सम्मत माना था. दशकों के अनुभव और सुप्रीम कोर्ट में आए अधिक मानहानि के मामलों की संख्या और प्रकरणों की प्रकृति देखकर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है, कि मानहानि को अपराध मुक्त बनाने का अब समय आ गया है.
न्यायालय ने महसूस किया कि तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण पुलिस कार्यवाही से कई व्यक्तियों को गहन पीड़ा पहुंचती है. कई मामलों में तो अदालत से पीड़ितों को न्याय मिला है. सोशल मीडिया के जमाने में ऐसे मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. शायद इसी कारण आपराधिक मानहानि में सुधार के लिए एक ऐसा वातावरण बना है.
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने भारत सरकार और संसद को यह अवसर दिया है कि इस पर विचार किया जाए. केंद्र सरकार लगातार अनुपयोगी कानूनों को समाप्त कर रही है. कानूनों में सुधार भी उनका एजेंडा रहा है. ऐसे में संसद ही अगर आपराधिक मानहानि के कानून को समाप्त करने की पहल करती है तो यह लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में बड़ा कदम होगा.
दुनिया के किसी देश में आपराधिक मानहानि का ऐसा कानून नहीं है. कुछ देशों में तो आपराधिक मानहानि को जारी रखने को दुनिया के सबसे दमनकारी शासन की श्रेणी में खड़ा करने के रूप में देखते हैं. सार्वजनिक विमर्श में राजनीतिज्ञों के खिलाफ जब भी अनियमितता या भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, तब आपराधिक मानहानि के कानून का सहारा लेकर आरोप लगाने वाले को अदालत में घसीटा जाता है. आरोप सही होने के बाद भी मानहानि के मुकदमे को राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है. मानहानि के मामले ज्यादातर राजनीतिक क्षेत्र में ही दिखाई पड़ते हैं. मीडिया में उनकी संख्या घटी है.
लोकतंत्र संवाद का ही तंत्र है. सहमति-असहमति खुलकर सामने आना चाहिए. ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए, कि किसी को भी अपने विचार व्यक्त करने में कानून या शासन के सिस्टम का भय लगे. जहां तक मानहानि का सवाल है, जब अन्य नागरिक कानूनों में इसकी समुचित व्यवस्था है, तो फिर आपराधिक मानहानि कानून की क्या आवश्यकता है.
ब्रिटिश राज से चला रहा अपराधिक मानहानि का कानून समाप्त होता है, तो यह लोकतंत्र के लिए अच्छा कदम होगा. संसद ने जैसे जेल से सरकार चलाने के खिलाफ कानून बनाने की पहल की है, वैसे ही आपराधिक मानहानि को समाप्त करने पर आगे बढ़ना चाहिए.
परिपक्व होते लोकतंत्र में यह अपेक्षा तो की ही जा सकती है कि जानबूझकर मानहानि का अपराध नहीं किया जाएगा.